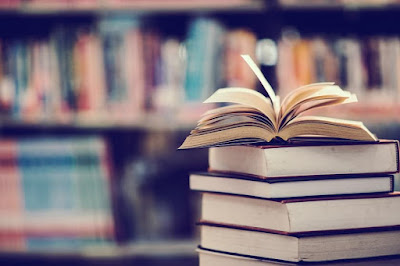 |
| BSEB Class 10 Hindi व्याकरण अपठित गद्यांश Textbook Solutions PDF: Download Bihar Board STD 10th Hindi व्याकरण अपठित गद्यांश Book Answers |
Bihar Board Class 10th Hindi व्याकरण अपठित गद्यांश Textbooks Solutions PDF
Bihar Board STD 10th Hindi व्याकरण अपठित गद्यांश Books Solutions with Answers are prepared and published by the Bihar Board Publishers. It is an autonomous organization to advise and assist qualitative improvements in school education. If you are in search of BSEB Class 10th Hindi व्याकरण अपठित गद्यांश Books Answers Solutions, then you are in the right place. Here is a complete hub of Bihar Board Class 10th Hindi व्याकरण अपठित गद्यांश solutions that are available here for free PDF downloads to help students for their adequate preparation. You can find all the subjects of Bihar Board STD 10th Hindi व्याकरण अपठित गद्यांश Textbooks. These Bihar Board Class 10th Hindi व्याकरण अपठित गद्यांश Textbooks Solutions English PDF will be helpful for effective education, and a maximum number of questions in exams are chosen from Bihar Board.Bihar Board Class 10th Hindi व्याकरण अपठित गद्यांश Books Solutions
| Board | BSEB |
| Materials | Textbook Solutions/Guide |
| Format | DOC/PDF |
| Class | 10th |
| Subject | Hindi व्याकरण अपठित गद्यांश |
| Chapters | All |
| Provider | Hsslive |
How to download Bihar Board Class 10th Hindi व्याकरण अपठित गद्यांश Textbook Solutions Answers PDF Online?
- Visit our website - Hsslive
- Click on the Bihar Board Class 10th Hindi व्याकरण अपठित गद्यांश Answers.
- Look for your Bihar Board STD 10th Hindi व्याकरण अपठित गद्यांश Textbooks PDF.
- Now download or read the Bihar Board Class 10th Hindi व्याकरण अपठित गद्यांश Textbook Solutions for PDF Free.
BSEB Class 10th Hindi व्याकरण अपठित गद्यांश Textbooks Solutions with Answer PDF Download
Find below the list of all BSEB Class 10th Hindi व्याकरण अपठित गद्यांश Textbook Solutions for PDF’s for you to download and prepare for the upcoming exams:Bihar Board Class 10 Hindi अपठित गद्यांश Questions and Answers
साहित्यिक गद्ययांश (300-400 शब्द)
1. देश-प्रेम है क्या? प्रेम ही तो है। इस प्रेम का आलंबन क्या है ? सारा देश अर्थात् मनुष्य, पशु, पक्षी, नदी, नाले, वन, पर्वत सहित सारी भूमि। यह प्रेम किस प्रकार का है ? यह साहचर्यगत प्रेम है। जिनके बीच हम रहते हैं, जिन्हें बराबर आँखों से देखते हैं, जिनकी बातें बराबर सुनते रहते हैं, जिनका हमारा हर घड़ी का साथ रहता है। सारांश यह है कि जिनके सान्निध्य का हमें अभ्यास पड़ जाता है, उनके प्रति लोभ या राग हो सकता है। देश-प्रेम यदि वास्तव में यह अंत:करण का कोई भाव है तो यही हो सकता है। यदि यह नहीं है तो वह कोरी बकवास या किसी और भाव के संकेत के लिए गढ़ा हुआ शब्द है।
यदि किसी को अपने देश से सचमुच प्रेम है तो उसे अपने देश के मनुष्य, पशु, पक्षी, लता, गुल्म, पेड़, पत्ते, वन, पर्वत, नदी, निर्झर आदि सबसे प्रेम होगा, वह सबको चाहभरी दृष्टि से देखेगा, वह सबकी सुध करके विदेश में आँसू बहाएगा। जो यह भी नहीं जानते कि कोयल किस चिड़िया का नाम है, जो यह भी नहीं सुनते कि चालक कहाँ चिल्लाता है, जो यह भी आँख भर नहीं देखते कि आम प्रणय-सौरभपूर्ण मंजरियों से कैसे लदे हुए हैं, जो यह भी नहीं झाँकते कि किसानों के झोंपड़ों के भीतर क्या हो रहा है, वे यदि दस बने-ठने मित्रों के बीच प्रत्येक भारतवासी की औसत आमदनी का पता बताकर देश-प्रेम का दावा करें तो उनसे पूछना चाहिए कि भाइयो! बिना रूप-परिचय का यह प्रेम कैसा? जिनके दुःख-सुख के तुम कभी साथी नहीं हुए, उन्हें तुम सुखी देखना चाहते हो, यह कैसे समझें। उनसे कोसों दूर बैठे-बैठे, पड़े-पड़े या खड़े-खड़े तुम विलायती बोली में “अर्थशास्त्र की दुहाई दिया करो, पर प्रेम का नाम उसके साथ न घसीटो।” प्रेम ।। हिसाब-किताब नहीं है। हिसाब-किताब करने वाले भाड़े पर भी मिल सकते हैं, पर प्रेम करने वाले नहीं।
हिसाब-किताब से देश की दशा का ज्ञानमात्र हो सकता है। हितचिंतन और हितसाधन की प्रवृत्ति कोरे ज्ञान से भिन्न है। वह मन के वेग या ‘भाव’ पर अवलंबित है, उसका संबंध लोभ या प्रेम से है, जिसके बिना अन्य पक्ष में आवश्यक त्याग का उत्साह हो नहीं सकता।
पशु और बालक भी जिनके साथ अधिक रहते हैं, उनसे परच जाते हैं। यह परचना परिचय ही है। परिचय प्रेम का प्रवर्तक है। बिना परिचय के प्रेम नहीं हो सकता। यदि-प्रेम के लिए हृदय में जगह करनी है तो देश के स्वरूप से परिचित और अभ्यस्त हो जाइए।
अपठित गद्यांश कक्षा 10 With Answer Bihar Board प्रश्न-
(क) इस गद्यांश का शीर्षक दीजिए।
(ख) ‘साहचर्यगत प्रेम’ से क्या आशय है-
- साथियों का प्रेम
- साथ-साथ हने के काण उत्पन्न प्रेम
- देश-प्रेम
- इनमें से कोई नहीं।
(ग) अंत:करण का एक पर्यायवाची लिखिए।
(घ) आँख भर देखना’ का आशय स्पष्ट कीजिए।
(ङ) ‘प्रेम हिसाब-किताब नहीं है’ में क्या व्यंग्य है ?
(च) देश-प्रेम का संबंध किससे है
- हिसाब-किताब से
- ज्ञान से
- मन के वेग से
- हितचिंतन से।
(छ) ‘परिचय प्रेम का प्रवर्तक है’ का क्या आशय है ?
(ज) देश-प्रेम के लिए पहली आवश्यकता क्या है ?
(झ) ‘देश-प्रेम’ का विग्रह करके समास का नाम लिखिए।
(ञ) वन’ के दो पर्यायवाची लिखिए।
(ट) ‘घड़ी’ के दो अर्थ लिखिए।
(ठ) निम्नलिखित वाक्य रचना की दृष्टि से किस प्रकार का है
हितसाधन और हितचिंतन की प्रवृत्ति कोरे ज्ञान से भिन्न है।
(ङ) निम्नलिखित वाक्य का अर्थ की दृष्टि से प्रकार बताइए-
इस प्रेम का आलंबन क्या है ?
उत्तर
(क) देश-प्रेम और स्वदेश-परिचय।
(ख) साथ-साथ रहने के कारण उत्पन्न प्रेम।
(ग) हृदय।
(घ) तृप्त होकर देखना, जी भरकर देखना।
(ङ) देश का हिसाब-किताब रखना अर्थात् आर्थिक उन्नति के बारे में सोचना देश-प्रेम की पहचान नहीं है।
(च) मन के वेग से।
(छ) परिचय से ही प्रेम का आरंभ होता है।
(ज) देश-प्रेम के लिए पहली आवश्यकता है देश को पूरी तरह जानना।
(झ) देश के लिए प्रेम; तत्पुरुष समास।
(ञ) कांतार, अरण्या
(ट) समय, समय देखने का यंत्र।
(ठ) सरल।
(ड) प्रश्नवाचका
2.गुरुदेव पूछते हैं कि भीष्म का अवतार क्यों नहीं माना गया। दिनकर जी महामना और उदार कवि थे। उनसे क्षमा मिल जाने की आशा से इतना तो कहा ही जा सकता है कि भीष्म अपने बम भोला नाथ गुरु परशुराम से अधिक संतुलित, विचारवान और ज्ञानी थे। पुराने रिकार्ड कुछ ऐसा सोचने को मजबूर कते है। फिर भी परशुराम को दस अवतारों में गिन लिया गया और बेचारे भीष्म को ऐसा कोई गौरव नहीं दिया गया। क्या कारण हो सकता है ?
एकांत में भीष्म सरकंडों की चटाई पर लेटे-लेटे क्या अपने बारे में सोचते नहीं होंगे? मेरा मन कहता है कि जरूर सोचते होंगे। भीष्म ने कभी बचपन में पिता की गलत आकांक्षाओं की तृप्ति के लिए भीषण प्रतिज्ञा की थी- वह आजीवन विवाह नहीं करेंगे। अर्थात् इस संभावना को ही नष्ट कर देंगे कि उनके पुत्र होगा और वह या उसकी संतान कुरुवंश के सिंहासन पर दावा करेगी। प्रतिज्ञा सचमुच भीषण थी। कहते हैं कि इस भीषण प्रतिज्ञा के कारण ही वह देवव्रत से “भीष्म” बने। यद्यपि चित्रवीर्य और विचित्रवीर्य तक तो कौरव-रक्त रह गया था तथापि बाद में वास्तविक कौरव-रक्त समाप्त हो गया, केवल कानूनी कौरव वंश चलता रहा। जीवन के अंतिम दिनों में इतिहास-मर्मज्ञ भीष्म को यह बात क्या खली नहीं होगी ?
भीष्म को अगर यह बात नहीं खली तो और भी बुरा हुआ। परशुराम चाहे ज्ञान-विज्ञान की जानकारी का बोझ ढोने में भीष्म के समकक्ष न रहे हों, पर सीधी बात को सीधे समझने में निश्चय ही वह उनसे बहुत आगे थे। वह भी ब्रह्मचारी थे-बालब्रह्मचारी। पर भीष्म जब अपने निर्वीर्य भाइयों के लिए कन्याहरण कर लाए और एक कन्या को अविवाहित रहने को बाध्य किया, तब उन्होंने भीष्म के इस अशोभन कार्य को क्षमा नहीं किया। समझाने-बुझाने तक ही नहीं रूके, लड़ाई भी की। पर भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के शब्दों में चिपटे ही रहे। वह भीष्म नहीं देख सके, वह लोक-कल्याण को नहीं समझ सके। फलतः अपहृता अपमानित कन्या जल मरी। नारद जी भी ब्रह्मचारी थे। उन्होंने सत्य के बार में शब्दों पर चिपटने को नहीं, सबके हित या कल्याण को अधिक जरूरी समझा था सत्यस्य वचनम् श्रेयः सत्यादपि हितं वदेत्।
भीष्म ने दसूरे पक्ष की उपेक्षा की थी। वह “सत्यस्य वचनम्” को “हित” से अधिक महत्त्व दं गए। श्रीकृष्ण ने ठीक इससे उलटा आचरण किया। प्रतिज्ञा में “सत्यस्य वचनम्” की अपेक्षा “हितम्” को अधिक महत्त्व दिया। क्या भारतीय सामूहिक चित्त ने भी उन्हें पूर्वावतार मानकर इसी पक्ष को अपना मौन समर्थन दिया है ? एक बार गलत-सही जो कह दिया, उसी से चिपट जाना “भीषण” हो सकता है, हितकर नहीं। भीष्म ने “भीषण” को ही चुना था।
Apathit Gadyansh Class 10 Bihar Board प्रश्न
(क) इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए।
(ख) परशुराम में कौन-सी विशेषता भीष्म से अधिक थी.?
(ग) भीष्म का नाम ‘भीष्म’ क्यों पड़ा?
(घ) भीष्म ने विवाह न करने की प्रतिज्ञा क्यों की थी?
(ङ) खलने’ का आशय स्पष्ट कीजिए।
(च) मनीषी’ के दो पर्यायवाची लिखिए।
(छ) ‘अपहरण की गई कन्या’ के लिए कौन-से शब्द का प्रयोग हुआ है ?
(ज) सत्यस्य वचनम्’ और ‘हितम्’ में कौन-सा महत्त्वपूर्ण है ?
(झ) कृष्ण ने वचन-सत्य और हित में से किसे चुना?
(ञ) भीष्म किस कमजोरी के कारण महान नहीं बन पाए ?
(ट)’बालब्रह्मचारी’ से क्या तात्पर्य है ?
(ठ) ‘लोक-कल्याण’ में कौन-सा समास है ?
(ड) आजीवन का विग्रह करके समास का नाम लिखिए।
(द) इस अनुच्छेद में प्रयुक्त अंग्रेजी शब्द छाँटिए।
(ण) विचारवान’ में प्रयुक्त प्रत्यय अलग कीजिए।
(त) संतुलित’ में कौन-सा उपसर्ग है ?
(थ) इत’ प्रत्यय से बने कोई दो शब्द छाँटिए।
उत्तर
(क) भीष्म की दुर्बलता।
(ख) परशुराम भीष्म की तुलना में सीधी बात को सीधे समझकर उसका वीरतापूर्वक मुकाबला करते थे।
(ग) भीष्म ने विवाह न करने की अत्यंत कठिन प्रतिज्ञा की थी। इसलिए उनका नाम भीष्म पड़ा।
(घ) पोभीष्म ने अपने पिता की अनुचित इच्छा को पूरा करने के लिए जीवन-भर अविवाहित रहने की कठोर प्रतिज्ञा की थी।
(ड) कष्ट देना, बुरा लगना।
(च) मनस्वी, मननशील, चिंतक।
(छ) अपहृत कन्या।
(ज) हितम्।
(झ) कृष्ण ने सत्य-वचन की बजाय हित-भावना को अधिक महत्त्व दिया।
(ञ) भीष्म ठीक समय पर ठीक निर्णय न ले पाने की कमजोरी के कारण महान नहीं बन पाए।
(ट) बचपन से ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करने वाला अर्थात् आजीवन संयम-नियम का पालन करते हुए अविवाहित रहने वाला व्यक्ति।
(ठ) तत्पुरुष।
(ड) जीवन रहने तक; अव्ययीभाव।
(ढ) रिकार्ड।
(ण) वान।
(त) सम्।
(थ) संतुलित, अपमानित।
3.एक आदमी को व्यर्थ बक-बक करने की आदत है। यदि वह अपनी आदत को छोड़ता है, तो वह अपने व्यर्थ बोलने के अवगुण को छोड़ता है। किंतु साथ ही और अनायास ही वह मितभाषी होने के सद्गुण को अपनाता चला जाता है। यह तो हुआ ‘हाँ’ पक्ष का उत्तर। किंतु एक-दूसरे आदमी को सिगरेट पीने का अभ्यास है। वह सिगरेट पीना छोड़ता है और उसके बजाय दूध से प्रेम करना सीखता है, तो सिगरेट पीना छोड़ना एक अवगुण को छोड़ना है और दूध से प्रेम जोड़ना एक सद्गुण को अपनाना है। दोनों ही भिन्न वस्तुएँ हैं-पृथक्-पृथक्।
अवगुण को दूर करने और सद्गुण को अपनाने के प्रयत्ल में, मैं समझता हूँ कि अवगुणों को दूर करने के प्रयत्नों की अपेक्षा सद्गुणों को अपनाने का ही महत्त्व अधिक है। किसी कमरे में गंदी हवा और स्वच्छ वायु एक साथ रह ही नहीं सकती। कमरे में हवा रहे ही नहीं, यह तो हो ही नहीं सकता। गंदी हवा को निकालने का सबसे अच्छा उपाय एक ही है सभी दरवाजे और खिड़कियाँ खोलकर स्वच्छ वायु को अंदर आने देना।
अवगुणों को भगाने का सबसे अच्छा उपाय है, सद्गुणों को अपनाना। ऐसी बातें पढ़-सुनकर हर आदमी वह बात कहता सुनाई देता है जो किसी समय बेचारे दुर्योधन के मुंह से निकली थी
“धर्म जानता हूँ, उसमें प्रवृत्ति नहीं।
अधर्म जानता हूँ, उससे निवृत्ति नहीं।”
एक आदमी को कोई कुटेव पड़ गई-सिगरेट पीने की ही सही। अत्यधिक सिनेमा देखने की ही सही। बेचारा बहुत संकल्प करता है, बहुत कसमें खाता है कि अब सिगरेट न पीऊंगा, अब सिनेमा देखने न जाऊँगा, किंतु समय आने पर जैसे आप-ही-आप उसके हाथ सिगरेट तक पहुँच
जाते हैं और सिगरेट उसके मुँह तक। बेचारे के पाँव सिनेमा की ओर जैसे आप-ही-आप बढ़े , चले जाते हैं।
क्या सिगरेट न पीने का और सिनेमा न देखने का उसका संकल्प सच्चा नहीं? क्या उसने झूठी कसम खाई है ? क्या उसके संकल्प की दृढ़ता में कमी है ? नहीं, उसका संकल्प तो उतना ही दृढ़ है जितना किसी का हो सकता है। तब उसे बार-बार असफलता क्यों होती है ? शायद असफलता का कारण इसी संकल्प में छिपा है। हम यदि अपने संकल्प-विकल्पों द्वारा अपने अवगुणों को बलवान न बनाएँ तो हमारे अवगुण
अपनी मौत आप मर जाएंगे।
आपकी प्रकृति चंचल है, आप अपने ‘गंभीर स्वरूप’ की भावना करें। यथावकाश अपने.मन में ‘गंभीर स्वरूप’ का चित्र देखें। अचिरकाल से ही आपकी प्रकृति बदल जाएगी।
Apathit Gadyansh In Hindi For Class 10 With Answers Bihar Board प्रश्न
(क) उचित शीर्षक दीजिए।
(ख) अनायास’ का अर्थ स्पष्ट कीजिए।
(ग) मितभाषी का विपरीतार्थक लिखिए।
(घ) पृथक्’ और ‘अभ्यास’ के कौन-कौन से पर्यायवाची शब्द प्रयुक्त हुए हैं ?
(ड) गंदी हवा को दूर करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है ?
(च) अवगुण को दूर करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है ?
(छ) धर्म जानता हूँ, उसमें प्रवृत्ति नहीं’ का आशय स्पष्ट कीजिए।
(ज) अवगुण कब अपनी मौत मर जाते हैं ?
(झ) लेखक अवगुणों को छोड़ने का संकल्प क्यों नहीं कराना चाहता?
(ञ) अधर्म जानता हूँ, उसमें निवृत्ति; नहीं’ का आशय स्पष्ट कीजिए। जादता
(ट) ‘तुरंत’ या ‘शीघ्र’ के लिए किस नए शब्द का प्रयोग किया गया है ?
(ठ) चंचल स्वभाव को छोड़ने के लिए क्या करना चाहिए?
(ड) ‘अनायास’ का संधिच्छेद कीजिए।
(द) अनायास, सद्गुण और प्रवृत्ति के विलोम लिखिए।
(ण) महत्त्व में प्रयुक्त प्रत्यय अलग कीजिए।
(त) ‘उत्तर’ के दो भिन्न अर्थ लिखिए।
(थ) ‘यथावकाश’ में कौन-सा समास है ?
(द) निम्नलिखित वाक्य किस प्रकार का है-
किसी कमरे में गंदी हवा और स्वच्छ वायु एक साथ रह ही नहीं सकती।
उत्तर
(क) सद्गुणों को अपनाने के उपाय।
(ख) बिना प्रयास किए, स्वयमेव।
(ग) अतिभाषी, वाचाल।
(घ) पृथक् – भिन्न
अभ्यास – आदत।
(ङ) गंदी हवा को दूर करने का सर्वोत्तम उपाय है-स्वच्छ हवा को आने देना।
(च) अवगुण को दूर करने का सर्वोत्तम उपाय है-सद्गुणों को अपनाना।
(छ) इसका आशय है-मैं धर्म के सारे लक्षण तो जानता हूँ, किंतु उस ओर मेरा रुझान नहीं है। मैं धर्म को अपनाने में रूचि नहीं ले पाता।
(ज) इसका आशय है-मैं अधर्म के लक्षण जानता हूँ किंतु जानते हुए भी उनसे बच नहीं पाता। मैं अधर्म के कार्यों में फंस जाता हूँ।
(झ) लेखक अवगुणों को छोड़ने का संकल्प इसलिए नहीं कराना चाहता क्योंकि उससे अवगुण और पक्के होते हैं। उससे अवगुण चिंतन के केंद्र में आ जाते हैं।
(ञ) अवगुणों के बारे में कोई निश्चय-अनिश्चय न किया जाए तो वे अपनी मौत स्वयं मर जाते हैं, अर्थात् अपने-आप नष्ट हो जाते हैं।
(ट) अचिरकला।
(ठ) चंचल स्वभाव को छोड़ने कवे लिए अपने सामने अपने गंभीर रूप की भावना करनी चाहिए।
(ड) अन् + आयास।
(ढ) अनायास – सायास।
सद्गुण – दुर्गुणा
प्रवृत्ति – निवृत्ति।
(ण) त्व।
(त) 1. जवाब,
2. एक दिशा का नाम।
(थ) अव्ययीभाव।
(द) सरल।
4. तुम्हें क्या करना चाहिए, इसका ठीक-ठीक उत्तर तुम्हीं को देना होगा, दूसरा कोई नहीं । दे सकता। कैसा भी विश्वास-पात्र मित्र हो, तुम्हारे इस काम को वह अपने ऊपर नहीं ले सकता। हम अनुभवी लोगों की बातों को आदर के साथ सुनें, बुद्धिमानों की सलाह को कृतज्ञतापूर्वक माने, पर इस बात को निश्चित समझकर कि हमारे कामों से ही हमारी रक्षा व हमारा पतन होगा, हमें अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को दृढ़तापूर्वक बनाए रखना चाहिए। जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है, उसका सिर कभी ऊपर न होगा। नीची दृष्टि रखने से यद्यपि रास्ते पर रहेंगे, पर इस बात को न देखेंगे कि यह रास्ता कहाँ ले जाता है। चित्त की स्वतंत्रता का मतलब चेष्टा की कठोरता या प्रकृति की उग्रता नहीं है। अपने व्यवहार में कोमल रहो और अपने उद्देश्यों को उच्च रखो, इस प्रकार नम्र और उच्चाशय दोनों बनो। अपने मन को कभी मरा हुआ न रखो। जो मनुष्य अपना लक्ष्य जितना ही ऊपर रखता है, उतना ही उसका तीर ऊपर जाता है।
संसार में ऐसे-ऐसे दृढ़ चित्त मनुष्य हो गए हैं जिन्होंने मरते दम तक सत्य को टेक नहीं छोड़ी, अपनी आत्मा के विरुद्ध कोई काम नहीं किया। राजा हरिश्चंद्र के ऊपर इतनी-इतनी । विपत्तियाँ आई, पर उन्होंने अपना सत्य नहीं छोड़ा। उनकी प्रतिज्ञा यही रही-
“चंद्र टरै, सूरज टरै, टरै जमत व्यवहारस
पै दृढ़ श्री हरश्चिंद्र को, टन सत्य विचार”
महाराणा प्रतापसिंह जंगल-जंगल मारे-मारे फिरते थे। अपनी स्त्री और बच्चों को भूख से तड़पते देखते थे, परंतु उन्होंने उन लोगों की बात न मानी जिन्होंने उन्हें अधीनतापूर्वक जीते रहने की सम्मति दी, क्योंकि वे जानते थे कि अपनी मर्यादा की चिंता जितनी अपने को हो सकती है, उतनी दूसरे को नहीं। एक इतिहासकार कहता है-“प्रत्येक मनुष्य का भाग्य उसके हाथ में है।” प्रत्येक मनुष्य अपना जीवन-निर्वाह श्रेष्ठ रीति से कर सकता है। यही मैंने किया है और यदि अवसर मिले तो यही करूँ।
इसे चाहे स्वतंत्रता कहो, चाहे आत्म-निर्भरता कहो, चाहे स्वावलंबन कहो, जो कुछ कहो, यह वही भाव है जिससे मनुष्य और दास में भेद जान पड़ता है, यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से राम-लक्ष्मण ने घर से निकल बड़े-बड़े पराक्रमी वीरों पर विजय प्राप्त की, यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से हनुमान ने अकेलें सीता की खोज की, यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से कोलंबस ने अमरीका समान बड़ा महाद्वीप ढूंढ़ निकाला। चित्त की इसी वृत्ति के बल पर कुंभनदास ने अकबर के बुलाने पर फतेहपुर सीकरी जाने से इनकार किया और कहा था
“मोको कहा सीकरी सो कामा”
इस चित्त-वृत्ति के बल पर मनुष्य इसलिए परिश्रम के साथ दिन काटता है और दरिद्रता के दुःख को झेलता है। इसी चित्त-वृत्ति के प्रभाव से हम प्रलोभनों का निवारण करके उन्हें सदा पद-दलित करते हैं, कुमंत्रणाओं का तिरस्कार करते हैं और शुद्ध चरित्र के लोगों से प्रेम और उनकी रक्षा करते हैं।
Apathit Gadyansh In Hindi For Class 10 Bihar Board प्रश्न
(क) उचित शीर्षक दीजिए।
(ख) लेखक नीची दृष्टि न रखने की सलाह क्यों देता है ?
(ग) नीची दृष्टि रखने के क्या लाभ हैं ?
(घ) मन को मरा हुआ रखने का क्या आशय है ?
(ङ) किसका तीर ऊपर जाता है और क्यों?
(च) ‘टेक’ के लिए किस पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया गया है?
(छ) ‘महाशय’ शब्द का समानार्थक शब्द इस अनुच्छेद से खोजिए।
(ज) महाराणा प्रताप ने गुलामी स्वीकार करने की सलाह क्यों नहीं मानी?
(झ) ‘विश्वासपात्र’, ‘निश्चित’ तथा ‘पतन’ के विलोम शब्द ढूंढिए।
(ञ) ‘सिर ऊपर होने’ का किसी वाक्य में प्रयोग कीजिए।
(ट) ‘सम्मति’ में कौन-सा उपसर्ग है ? ।
(ठ) ‘दृष्टि नीची होने’ का आशय स्पष्ट कीजिए।
(ड) ‘आत्म-निर्भरता’ का पर्यायवाची शब्द खोजिए।
(ढ) कोलंबस और हनुमान ने किस गुण के बल पर महान कार्य किए?
(ण) मनुष्य किस आधार पर प्रलोभनों को पद-दलित कर पाते हैं?
(त) अज्ञता’ और ‘आलंबन’ की जगह किसी समानार्थक शब्द को रखिए।
(थ) योग्य, समर्थ, क्षमतावान तथा सार्थक में से कौन-सा शब्द शेष शब्दों का पर्यायवाची नहीं है।
(द) श्रेष्ठ, उत्तम, उच्च और दृढ़ में से अलग अर्थ वाला शब्द अलग कीजिए। (घ) राम-लक्ष्मण’ का विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। उत्तर
(क) आत्मनिर्भरता की महिमा।
(ख) नीची दृष्टि रखने से मनुष्य न तो उन्नति कर पाता है और न ही उच्च दिशा की ओर पाँव रख पाता है।
(ग) नीची दृष्टि का लाभ यह है कि इससे मनुष्य सदा सही रास्ते पर चलता रहता है।
(घ) मन को उत्साहहीन, निराश, उदास और पराजित बनाए रखना।
(ङ) जिसका लक्ष्य जितना ऊँचा होता है, उसका तीरे उतना ही ऊपर जाता है। लक्ष्य ऊँचा रखने से ऊपर बढ़ने के अवसर प्राप्त होते हैं।
(च) प्रतिज्ञा।
(छ) उच्चाशय।
(ज) महाराणा प्रताप जानते थे कि व्यक्ति को अपनी मर्यादा स्वयं अपने कर्म से बनानी होती है। इसलिए उन्होंने उन मित्रों की सलाह नहीं मानी जिन्होंने उन्हें परतंत्रता स्वीकार करने की सलाह दी।
(झ) विश्वासपात्र – विश्वासघाती
निश्चित – अनिश्चित
पतन – उत्थान
(ञ) अच्छे चरित्र के लोगों का सिर सदा ऊपर रहता है।
(ट) सम्।
(ठ) छोटा लक्ष्य रखना।
(ड) स्वावलंबन, स्वतंत्रता।
(ढ) आत्मनिर्भरता के बल पर।
(ण) आत्मनिर्भरता के आधार पर।
(त) अज्ञता – अज्ञानता
आलंबन – सहारे।
(थ) सार्थका
(द) दृढ़।
(ध) ‘राम और लक्ष्मण’; द्वंद्व समास।
5. हम जिस तरह भोजन करते हैं, गाछ-बिरछ भी उसी तरह भोजन करते हैं। हमारे दाँत हैं, कठोर चीज खा सकते हैं। नन्हे बच्चों के दाँत नहीं होते। वे केवल दूध पी सकते हैं। गाछ-बिरछ के भी दाँत नहीं होते, इसलिए वे केवल तरल द्रव्य या वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। गाछ-बिरछ जड़ के द्वारा माटी से रसपान करते हैं। चीनी में पानी डालने पर चीनी गल जाती है। माटी में पानी डालने पर उसके भीतर बहुत-से द्रव्य गल जाते हैं। गाछ-बिरछ वे ही तमाम द्रव्य सोखते हैं। जड़ों को पानी न मिलने पर पेड़ का जन बंद हो जाता है, पेड़ मर जाता है।
खुर्दबीन से अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ स्पष्टतया देखे जा सकते हैं। प्रेड़ की डाल अथवा जड़ का इस यंत्र द्वारा परीक्षण करके देखा जा सकता है कि पेड़ में हजारों-हजार नल हैं। इन्हीं सब नलों के द्वारा माटी से पेड़ के शरीर में रस का संचार होता है।
इसके अलावा गाछ के पत्ते हवा से आहार ग्रहण करते हैं। पत्तों में अनगिनत छोटे-छोटे मुँह होते हैं। खुर्दबीन के जरिए अनगिनत मुंह पर अनगिनत होंठ देखे जा सकते हैं। जब आहार करने की जरूरत न हो तब दोनों होंठ बंद हो जाते हैं। जब हम श्वास लेते हैं और उसे बाहर निकालते हैं तो एक प्रकार की विषाक्त वायु बाहर निकलती है उसे ‘अंगारक’ वायु कहते हैं। अगर यह जहरीली हवा पृथ्वी पर इकट्ठी होती रहे तो तमाम जीव-जंतु कुछ ही दिनों में उसका सेवन करके नष्ट हो सकते हैं।
“जरा विधाता की करुणा का चमत्कार तो देखो-जो जीव-जंतुओं के लिए जहर है, गाछ-बिरछ उसी का सेवन करके उसे पूर्णतया शुद्ध कर देते हैं। पेड़ के पत्तों पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तब पत्ते सूर्य ऊर्जा के सहारे ‘अंगारक वायु से अंगार निःशेष कर डालते हैं। और यही अंगार बिरछ के शरीर में प्रवेश करके उसका संवर्द्धन करते हैं।” पेड़-पौधे प्रकाश चाहते हैं। प्रकाश न मिलने पर बच नहीं सकते। गाछ-बिरछ की सर्वाधिक कोशिश यही रहती है कि किसी तरह उन्हें थोड़ा-सा प्रकाश मिल जाए। यदि खिड़की के पास गमले में पौधे रखो, तब देखोगे कि सारी पत्तियाँ व डालियाँ अंधकार से बचकर प्रकाश की ओर बढ़ रही हैं। वन में जाने पर पता लगेगा कि तमाम गाछ-बिरछ इस होड़ में सचेष्ट हैं कि कौन जल्दी से सर उठाकर पहले प्रकाश को झपट ले। बेल-लताएँ छाया में घड़ी हने से प्रकाश के अभाव में मर जाएंगी। इसीलिए वे पेड़ों से लिपटती हुई, निरंतर ऊपर की ओर अग्रसर होती रहती हैं।
अब तो समझ गए होंगे कि प्रकाश ही जीवन का मूलमंत्र है। सूर्य-किरण का परस पाकर ही पेड़ पल्लवित होता है। गाछ-बिरछ के रेशे-रेशे में सूरज की किरणें आबद्ध हैं। ईंधन को जलाने पर जो प्रकाश व ताप बाहर प्रकट होता है वह सूर्य की ही ऊर्जा है।
Class 10 Apathit Gadyansh Bihar Board प्रश्न
(क) उचित शीर्षक दीजिए।
(ख) ‘गाछ-बिरछ’ का क्या अर्थ है ?
(ग) गाछ-बिरछ किस प्रकार भोजन ग्रहण करते हैं ?
(घ) वृक्ष वायु का सेवन किस प्रकार करते हैं ?
(ङ) वृक्ष जल किस प्रकार पीते हैं ?
(च) पेड़ की मृत्यु कब होती है?
(छ) . ‘अंगारक वायु’ किसे कहते हैं ?
(ज) ‘कोशिश’ तथा ‘तमाम’ के लिए तत्सम शब्द बताइए।
(झ) ‘गाछ-बिरछ’ शब्द-युग्म के लिए और कौन-सा शब्द-युग्म प्रयुक्त किया गया है ?
(ञ) गाछ-बिरछ और हरियाली सूरज के प्रकाश को हथियाने के जाल हैं कैसे?
(ट) ‘संवर्द्धन’ में कौन-सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है ? ‘
(ठ) ‘उत्सुक’, ‘व्याकुल’ के लिए किस पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया गया है ?
(ड) ‘सर्य’ के दो पर्यायवाची लिखिए।
(ढ) ‘श्वास’ का तदभव लिखिए।
(ण) स्नेहसिक्त वाणी का अर्थ स्पष्ट कीजिए।
(त) ‘गाछ-बिरछ’ और ‘सूर्य-किरण’ में कौन-सा समास है ?
(थ) ‘छोटे-छोटे का विग्रह करके समास का नाम लिखिए।
उत्तर-
(क) पेडों का जीवन।
(ख) पेड-पौधे।
(ग) गाछ-बिरछ जल और वायु द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं।
(घ) – वृक्ष के पत्तों पर असंख्य मुंह होते हैं। वे उन्हीं के द्वारा साँस लेकर वायु का सेवन करते हैं।
(ङ) वृक्ष जड़ों और डालों में उगे असंख्य नलों द्वारा जल ग्रहण करते हैं।
(च) जड़ों को पानी न मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है। इस कारण पेड़ की मृत्यु हो जाती है।
(छ) मुंह से निकलने वाली साँस के साथ निकलने वाली वायु को ‘अंगारक वायु’ कहते हैं। :
(ज)कोशिश – प्रयत्न
‘तमाम – समस्त, संपूर्ण, सारा।
(झ) पेड़-पौधे।
(ञ) पेड़-पौधे और हरियाली सूर्य की गर्मी को सोखकर अपने अंदर सुरक्षित रखते हैं। अत एक प्रकार से ये सूरज के प्रकाश को हथियाने के जाल हैं।
(ट) सम्।
(ठ) व्यग्र।
(ड) सूरज, दिनकर।
(ण) स्नेह से सनी हुई वाणी।
(त) गाछ-बिरछ – द्वंद्व समास।
‘सूर्य-किरण – तत्पुरुष समास
(थ)बहुत छोटे; अव्ययीभाव समास।
6. मानव के लिए विचार अथवा अनुभव में जो कुछ भी श्रेष्ठ है, उदात्त है, वह इसका अथवा उसका नहीं है, जातिगत अथवा देशगत नहीं है, वह सबका है, सारे विश्व का है। समस्त ज्ञान, विज्ञान और सभ्यता सारी मानवता की विरासत है। भले ही एक विचार का जन्म किसी अन्य देश में भिन्न भाषा-भाषी लोगों के द्वारा हुआ हो, वह हमारा भी है, सबका है। पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के भेद निराधार हैं। महापुरुष विरोधी नहीं होते हैं, एक-दूसरे के पूरक होते हैं। महापुरुषों में अपने देश की विशेषताएँ होती हैं। विवेकशील मनुष्य नम्रतापूर्वक महापुरुषों से शिक्षा ग्रहण कर अपने जीवन को प्रकाशित करने का प्रयत्न कता है। समस्त मानवता उसके प्रति कृतज्ञ है। किंतु अब हमें उनसे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ज्ञान की इतिश्री नहीं होती है तथा किसी का शब्द अंतिम नहीं होता है।
संसार एक खुली पाठशाला है, जीवन एक खुली पुस्तक है। सदैव सीखते रहना चाहिए तथा सीखना ही आगे पढ़ने के लिए नए रास्ते खोलता है। विकास की क्रिया के मूल में मानव की पूर्ण बनने की अपनी प्रेरणा है। विकास के लिए समन्वय का भाव होना परम आवश्यक होता है। यदि हम विभिन्न विचारधाराओं एवं उनके जन्मदाता महापुरुषों का पूर्ण . खंडन अथवा पूर्ण मंडन करें तो विकास पथ अवरुद्ध हो जाएगा। अतएव समन्वय की भावना से युक्त होकर सब ओर से सारी वस्तुओं को ग्रहण करते हुए हम उनका लाभ उठा सकते हैं। किसी धर्म विशेष या मान्यता के खूटे के साथ संकीर्ण भाव से बंधकर तथा परंपराओं और रूढ़ियों से जकड़े हुए हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं।
मानव को मानव रूप में सम्मानित करके ही हम जातीयता, प्रांतीयता, क्षुद्र राष्ट्रीयता के भेद को तोड़ सकते हैं। आज मानव मानव से दूर हटता जा रहा है। वह भूल चुका है कि देश, धर्म और जाति के भिन्न होते हुए भी हम सर्वप्रथम मानव हैं और समान हैं तथा सभी की भावनाएँ और लक्ष्य एक ही हैं। आज. धर्म, सत्ता, धन आदि का भेद होने से एक मानव दूसरे मानव को मानव ही नहीं मानता है। कभी-कभी स्वधर्मी-विधर्मी को, स्वदेशी-विदेशी को; अफसर चपरासी को, धनी निर्धन को तथा विद्वान निरक्षर को इन्सान ही नहीं समझता है और भूल जाता है कि दूसरे को भी समान रूप से इच्छानुसार भूख और प्यास सताते हैं तथा उसे भी प्रेम और आदर चाहिए। वह भूल जाता है कि दूसरे में भी स्वाभिमान का पुट है, उसे भी विश्राम की आवश्यकता ‘ है और उसे भी अपने बच्चे प्रिय हैं अथवा वह भी अपनी संतान के लिए कुछ करना चाहता है।
अपठित गद्यांश एवं पद्यांश कक्षा 10 Bihar Board प्रश्न
(क) शीर्षक लिखिए।
(ख) विरासत का क्या अर्थ है ? इसका पर्यायवाची शब्द बताइए।
(ग) ‘महापुरुष विरोधी नहीं, एक-दूसरे के पूरक होते हैं’-आशय स्पष्ट कीजिए।
(घ) संसार को खुली पाठशाला कहकर लेखक क्या प्रेरणा देना चाहता है ?
(ङ) मनुष्य किस प्रेरणा से विकास करता है?
(च) विकास के लिए किस गुण का होना आवश्यक है ?
(छ) ‘समन्वय’ से क्या आशय है ?
(ज) हर प्रकार के भेद को तोड़ने का क्या उपाय है?
(झ) एक मानव दूसरे मानव को मानव क्यों नहीं मानता ?
(ञ) ‘अवरुद्ध’ तथा ‘समन्वय’ में प्रयुक्त उपसर्ग अलग कीजिए।
(ट) ‘आज मानव मानव से दूर हटता जा रहा है रचना की दृष्टि से यह किस प्रकार , का वाक्य है?
(ठ) ‘जातीयता’ तथा ‘राष्ट्रीयता’ में प्रयुक्त प्रत्यय अलग कीजिए।
(ड) ‘खंडन’, ‘धनी’ और ‘विद्वान’ के विलोम लिखिए।
(ढ) ‘इतिश्री होने’ का आशय स्पष्ट कीजिए।
(ण) ‘भेद’ के दो अर्थ लिखिए।
(त) ‘नौकर’ तथा ‘विश्व’ के दो-दो पर्यायवाची बताइए।
(थ) ‘भू-भाग’ तथा ‘पाठशाला’ का विग्रह करके समास का नाम लिखिए।
(द) ‘निरक्षर’ में कौन-सा समास है ?
उत्तर
(क) मानव-धर्म।
(ख) माता-पिता या परंपरा से मिली संपत्ति या संस्कारों को विरासत कहते हैं। इसका पर्यायवाची है उत्तराधिकार।
(ग) महापुरुष एक-दूसरे का विरोध नहीं करते। वे एक-दूसरे की कमियों को पूरा करने
की चेष्य करते हैं।
(घ) संसार को खुली पाठशाला कहकर लेखक जीवन-भर नया कुछ सीखने की प्रेरणा देना चाहता है।
(ड) मनुष्य स्वयं को पूर्ण बनाने की प्रेरणा से विकास करता है।
(च) विकास के लिए समन्वय अर्थात् तालमेल का होना आवश्यक है। तालमेल; भिन्नता रखने वालों में मेल बैठाना।
(छ) मानव को मानव के रूप में सम्मानित करके ही सब प्रकार के भेद तोड़े जा सकते हैं।
(झ) धर्म, सत्ता या धन का भेद होने के कारण एक मानव दूसरे मानव को मानव नहीं मानता।
(ञ) अवरुद्ध – अवा
समन्वय – सम्।
(ट) सरल वाक्य।
(ठ) इय + ता।
खंडन – मंडन
(ड) धनी – निर्धन
विद्वान – निरक्षर।
(ढ) समाप्त होना, नष्ट होना।
(ण) 1. रहस्य
2. प्रकार।
(त) नौकर – भृत्य, दास
विश्व – जग, संसार।
(थ) भू का भागः तत्पुरुष समास।
पाठ के लिए शाला; तत्पुरुष समास।
(द) जिसे अक्षर-ज्ञान नहीं; नञ् तत्पुरुष।
7. यदि साहित्य समाज का दर्पण होता तो संसार को बदलने की बात न उठती। कवि का काम यथार्थ जीवन को प्रतिबिंबित करना ही होता तो वह प्रजापति का दर्जा न पाता। वास्तव में प्रजापति ने जो समाज बनाया है, उससे असंतुष्ट होकर नया समाज बनाना कवि का जन्मसिद्ध अधिकार है।
कवि की यह सृष्टि निराधार नहीं होती। हम उसमें अपनी ज्यों-की-त्यों आकृति भले ही न देखें, पर ऐसी आकृति जरूर देखते हैं जैसी हमें प्रिय है, जैसी आकृति हम बनाना चाहते हैं। कवि अपनी रूचि के अनुसार जब विश्व को परिवर्तित करता है तो यह भी बताता है कि विश्व से उसे असंतोष क्यों है। वह यह भी बताता है कि विश्व में उसे क्या रूचता है जिसे वह फलता-फूलता देखना चाहता है। उसके चित्र के चमकीले रंग और पार्श्व-भूमि की गहरी काली रेखाएँ—दोनों ही यथार्थ जीवन से उत्पन्न होते हैं। इसलिए प्रजापति कवि गंभीर यथार्थवादी होता है, ऐसा यथार्थवादी जिसके पाँव वर्तमान की धरती पर हैं और आँखें भविष्य के क्षितिज पर लगी हुई है।
इसलिए मनुष्य साहित्य में अपने सुख-दुःख की बात ही नहीं सुनता, वह उसमें आशा का स्वर भी सुनता है। साहित्य थके हुए मनुष्य के लिए विश्रांति ही नहीं है, वह उसे आगे बढ़ने के लिए उत्साहित भी करता है।
पंद्रहवीं-सोलहवीं सदी में हिंदी साहित्य ने यही भूमिका पूरी की थी। सामंती पिंजड़े में बंद मानव-जीवन की मुक्ति के लिए उसने वर्ण और धर्म के सींकचों पर प्रहार किए थे। कश्मीरी ललदेद, पंजाबी नानक, हिंदी सूर-तुलसी-मीरा-कबीर, बंगाली चंडीदास, तमिल तिरुवल्लुवर आदि-आदि गायकों ने भागे-पीछे समूचे भारत में उस जीर्ण मानव-संबंधों के पिंजड़े को झकझोर दिया था। इन गायकों की वाणी ने पीड़ित जनता के मर्म को स्पर्श कर उसे नए जीवन के लिए बटोरा, उसे आशा दी, उसे संगठित किया और जहाँ-तहाँ जीवन को बदलने के लिए संघर्ष के लिए आमंत्रित भी किया।
सत्रहवीं और बीसवीं सदी में बंगाली रवींद्रनाथ, हिंदी भारतेंदु, तेलगु वीरेशलिंगम्, तमिल भारती, मलयाली वल्लतोल आदि-आदि ने अंग्रेजी राज और सामंती अवशेषों के पिंजड़े पर फिर प्रहार किया। एक बार फिर उन्होंने भारत की दुःखी पराधीन जनता को बटोरा, उसे संगठित किया, उसकी मनोवृत्ति बदली, उसे सुखी स्वाधीन जीवन की तरफ बढ़ने के लिए उत्साहित किया।
साहित्य का पांचजन्य समर-भूमि में उदासीनता का राग नहीं सुनाता। वह मनुष्य को भाग्य के आसरे बैठने और पिंजड़े में पंख फड़फड़ाने की प्रेरणा नहीं देता। इस तरह की प्रेरणा देने वालों के वह पंख कतर देता है। वह कायरों और पराभव प्रेमियों को ललकारता हुआ एक बार उन्हें । भी समर-भूमि में उतरने के लिए बुलावा देता है।
अपठित गद्यांश कक्षा 10 के लिए Bihar Board प्रश्न
(क) उचित शीर्षक दीजिए।
(ख) ‘साहित्य समाज का दर्पण है’-आशय स्पष्ट कीजिए।
(ग) कवि अपनी कविता द्वारा क्या करना चाहता है ?
(घ) कवि दर्पणकार नहीं, प्रजापति है-आशय स्पष्ट कीजिए।
(ङ) प्रजापति के दो पर्यायवाची लिखिए।
(च) असंतुष्ट’ में किन उपसर्गों का प्रयोग हुआ है ?
(छ) “पराधीन’ का विलोम लिखिए।
(ज) कवि को प्रजापति बनने की जरूरत क्यों पड़ती है ?
(झ) निम्नलिखित वाक्य का भेद बताइए कवि जब अपनी रुचि के अनुसार विश्व को परावर्तित करता है तो यह भी बताता है कि विश्व में उसे असंतोष क्यों है ?
(ञ) ‘पंख फड़फड़ाने’ का क्या आशय है ?
(ट) प्राचीन संत कवियों ने कौन-सा महत्त्वपूर्ण कार्य किया ?
(ठ) रवींद्रनाथ, भारतेंदु आदि कवियों ने किस पर चोट की?
(ड) बीसवीं सदी के साहित्यकारों ने समाज को किसलिए उत्साहित किया?
(ढ) युद्ध और संगीत के लिए कौन-से शब्दों का प्रयोग हुआ है ?
(ण)’पंख फड़फड़ाने’ का विपरीतार्थक मुहावरा कौन-सा है?
(त) ‘पंख कतरना’ का अर्थ स्पष्ट कीजिए।
(थ) ‘साहित्य का पांचजन्य’ में कौन-सा अलंकार है ?
(द) ‘मानव-संबंध’ में कौन-सा समास है ?
उत्तर
(क) कवि : समाज-निर्माता।
(ख) इसका आशय है साहित्य में समाज का सच्चा रूप झलकता है।
(ग) कवि अपनी कविता द्वारा नया और सुंदर समाज बनाना चाहता है।
(घ) कवि केवल समाज का ज्यों-का-त्यों चित्रण ही नहीं करता, अपितु उसका नव-निर्माण करता है।
(ङ) विधाता, रचयिता।
(च) अ, सम्।
(छ) स्वाधीन।
(ज) कवि मानव-संबंधों में कमी देखकर उसे अपनी कल्पना और रचना-शक्ति से ठीक करना चाहता है। इसलिए उसे प्रजापति बनने की आवश्यकता पड़ती है।
(झ) मिश्र वाक्या
(ब) मुक्ति के लिए प्रयत्न करना।
(ट) प्राचीन संत कवियों ने मानव-संबंधों में आई जड़ता को तोड़ा तथा पीड़ित जनता को , संघर्ष के लिए प्रेरित किया।
(ठ) रवींद्रनाथ, भारतेंदु आदि कवियों ने अंग्रेजी राज और सामंती प्रथा पर चोट की।
(ड) बीसवीं सदी के साहित्यकारों ने समाज को स्वाधीनता के लिए उत्साहित किया।
(ढ) युद्ध – समर
संगीत – राग
(ण) पंख कतरना।
(त) किसी उत्साही के उत्साह को नष्ट कर देना।
(थ) रूपका
(द) तत्पुरुष समास।
8. शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि ‘वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे, सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई और जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्त्वपूर्ण ‘ पद प पहुंचे, तब भी वह सामान्य ही बने रहे।’ विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व
में एक विचित्र प्रकार का आकर्षण पैदा करती थी। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था और कहना न होगा कि बापू से प्रभावित होकर ही सन् 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ी थी। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों, डॉ. भगवानदास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन-भर उन्हीं के आदर्शों पर चलते रहे तथा औरों को इसके लिए प्रेरित करते रहे। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबिल की वह उक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे।
शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया था, जब वे एक स्कूल में विद्यार्थी थे ओर उस समय उनकी उम्र 17 वर्ष की थी। गाँधी जी के आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। उनका मन हमेशा देश की आजादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहा। परिणाम यह हुआ कि सन् 1926 में वे ‘लोक सेवा मंडल’ में शामिल हो गए, जिसके वे जीवन-भर सदस्य रहे। इसमें शामिल होने के बाद से शास्त्री जी ने गाँधी जी के विचारों के अनुरूप अछूतोद्धार के काम में अपने आपको लगाया। यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो गया।
सन् 1930 में जब ‘नमक कानून तोड़ो आंदोलन’ शुरू हुआ, तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया जिसके परिणामस्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा। यहाँ से शास्त्री जी की जेल-यात्रा की जो शुरूआत हुई तो वह सन् 1942 के ‘भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही। इन 12 वर्षों के दौरान वे सात बार जेल गए। इसी से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आजादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी। दूसरी जेल-यात्रा उन्हें सन् 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी। सन् 1942 की उनकी जेल-यात्रा 3 वर्ष की थी, जो सबसे लंबी जेल-यात्रा थी।
इस दौरान शास्त्री जी जहाँ एक ओर गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जनसेवा के कार्यों में भी लगे रहे। इसके बाद के 6 वर्षों तक वे इलोहाबाद की नगरपालिका से किसी-न-किसी रूप में जुड़े रहे। लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी-छोटी समस्याओं और उनके निराकरण की व्यावहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हो गए थे। कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण सन् 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। सही मायने में यहीं से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरूआत हुई, जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में हुआ।
Apathit Gadyansh In Hindi For Class 10 With Bihar Board प्रश्न
(क) उपयुक्त शीर्षक दीजिए।
(ख) शास्त्री जी के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी?
(ग) शास्त्री के व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने वाले गुण कौन-कौन से थे?
(घ) ‘विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विचित्र प्रकार का आकर्षण पैदा करती थी।’ रेखांकित शब्दों से विशेषण बनाइए।
(ङ) किस गुण के कारण शास्त्री जी का जीवन गाँधी जी के करीब था?
(च) ‘विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे’ का क्या आशय है?
(छ) शास्त्री जी ने स्वतंत्रता-आंदोलन में भाग लेने की शुरूआत कब से की?
(ज) शास्त्री जी 1942 में किस सिलसिले में जेल गए?
(झ) इस अनुच्छेद से तत्सम तथा उर्दू के दो-दो शब्द छाँटिए।
(ञ) ‘ललक’ के दो पर्यायवाची लिखिए।
(ट) शास्त्री जी ने जनसेवक के रूप में किस नगर की सेवा की?
(ठ) कौन-से सन् में शास्त्री जी संसद सभा के सदस्य बने ?
(ड) ‘अछूतोद्धार’ का विग्रह करके समास का नाम लिखिए।
उत्तर-
(क) कर्मयोगी लालबहादुर शास्त्री।
(ख) शास्त्री जी के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता थी, उनकी सादगी और सरलता।
(ग) शास्त्री जी के व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने वाले गुण थे-विनम्रता, सादगी और सरलता
(घ) विनम्रता – विनम्र
सादगी – सादा
सरलता – सरल
आकर्षण आकर्षक
(ङ) सादगी और सरलता के कारण।
(च) पृथ्वी के अंत में विनम्र लोग ही बचेंगे। वे ही धरती के सब सुखों का भोग करेंगे।
(छ) 17 वर्ष की उम्र में विद्यार्थी-जीवन से।
(ज) भारत छोड़ो आंदोलन के सिलसिले में।
(झ) तत्सम रचनात्मक, महत्वपूर्ण
उर्दू – वारिस, परवरिश
(ञ) उत्सुकता, व्यग्रता।
(ट) इलाहाबाद नगरपालिका की।
(ठ) सन् 1937 में।
(ड) अछूतों का उद्धार; तत्पुरुष समास।
9. एक बार मैंने एक बुड्ढे गड़रिये को देखा। घना जंगल है। हरे-हरे वृक्षों के नीचे उसकी सफेद ऊन वाली भेड़ें अपना मुँह नीचे किए हुए कामल-कोमल पत्तियाँ खा रही हैं। गड़रिया बैठा आकाश की ओर देख रहा है। ऊन कातता जाता है। उसकी आँखों में प्रेम-लाली छाई हुई है। वह निरोगता की पवित्र मदिरा से मस्त हो रहा है। बाल उसके सारे सफेद हैं। और क्यों न सफेद हों? सफेद भेड़ों का मालिक जो ठहरा। परंतु उसके कपोलों से लाली फूट रही है। बरफानी देशों में वह मानो विष्णु के समान क्षीरसागर में लेटा है। उसकी प्यारी स्त्री उसके पास रोटी पका रही है। उसकी दो जवान कन्याएँ उसके साथ जंगल-जंगल भेड़ चराती घूमती हैं। अपने माता-पिता और भेड़ों को छोड़कर उन्होंने किसी और को नहीं देखा। मकान इनका बेमकान है, घर इनका बेघर है, ये लोग बेनाम और बेपता हैं।
इस दिव्य परिवार को कुटी की जरूरत नहीं। जहाँ जाते हैं, एक घास की झोपड़ी बना लेते हैं। दिन को सूर्य रात को तारागण इनके सखा हैं।।
गड़रिये की कन्या पर्वत के शिखर के ऊपर खड़ी सूर्य का अस्त होना देख रही है। उसकी सुनहली किरणें इसके लावण्यमय मुख पर पड़ रही हैं। यह सूर्य को देख रही है और वह इसको देख रहा है।
हुए थे आँखों के कल इशारे इधर हमारे उधर तुम्हारे।
चले थे अश्कों के क्या फव्वारे इधर हमारे उधर तुम्हारे।।
बोलता कोई भी नहीं। सूर्य उनकी युवावस्था की पवित्रता पर मुग्ध है और वह आश्चर्य के अवतार सूर्य की महिमा के तूफान में पड़ी नाच रही है।
इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंधि से सुगंधित है। इनके मुख, शरीर और अंत:करण सफेद, इनकी बर्फ, पर्वत और भेड़ें सफेद। अपनी सफेद भेड़ों में यह परिवार शुद्ध सफेद ईश्वर के ‘दर्शन करता है।
जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूँ तुमको
मैं तो देखता हूँ तुमको जो खुदा को देखना हो।
भेड़ों की सेवा ही इनकी पूजा है। जरा एक भेड़ बीमार हुई, सब परिवार पर विपत्ति आई। दिन-रात उसके पास बैठे काट देते हैं। उसे अधिक पीड़ा हुई तो इन सब की आँखें शून्य आकाश में किसी को देखने लग गई। पता नहीं ये किसे बुलाती हैं। हाथ जोड़ने तक की इन्हें फुरसत नहीं। पर हाँ, इन सब की आँखें किसी के आगे शब्द-रहित संकल्प-रहित मौन प्रार्थना में खुली हैं। दो रातें इसी तरह गुजर गई। इनकी भेड़ अब अच्छी है। इनके घर मंगल हो रहा है। सारा परिवार मिलकर गा रहा है।
इतने में नीले आकाश पर बादल घिर और झम-झम बरसने लगे। मानां प्रकृति के देवता भी इनके आनंद से आनंदित हुए। बूढा गड़रिया आनंद-मत्त होकर नाचने लगा। वह कहता कुछ नहीं, रग-रग उसकी नाच रही है। पिता को ऐसा सुखी देख दोनों कन्याओं ने एक-दूसरं का हाथ पकड़कर राग अलापना आरंभ कर दिया जाता। साथ ही धम-धम थम-थम नाच की उन्होंने धूम मचा दी। मेरी आँखों के सामने ब्रह्मानंद का समाँ बाँध दिया।
Apathit Gadyansh In Hindi Bihar Board प्रश्न
(क) उचित शीर्षक दीजिए।
(ख) गड़रिये के परिवार में कौन-कौन सदस्य हैं?
(ग) गड़रिये का मकान कैसा है ?
(घ) लेखक ने किस ‘दिव्य परिवार’ कहा है और क्यों?
(ङ) ‘लावण्यमय’ का अर्थ स्पष्ट कीजिए।
(च) गड़रिये के परिवार के सदस्य विपत्ति पड़ने पर किसकी आराधना करते हैं?
(छ) गड़रिया किस कारण आनंद से नाचने लगा?
(ज) ‘ब्रह्मानंद का समाँ बाँधना’ का आशय स्पष्ट कीजिए।
(झ) इस अनुच्छेद से दो विशेषण खोजिए।
(ञ) ‘स्त्री’ के दो भिन्न अर्थ लिखिए।
(ट) युवावस्था का विग्रह करके समास का नाम लिखिए।
(ठ) इस अनुच्छेद से दो उर्दू तथा दो तत्सम शब्द छाँटिए।
(ड) ‘पंडित’ शब्द का पर्यायवाची लिखिए।
(ढ) लेखक अज्ञान और ज्ञान में से किसे स्वीकार करना चाहता है ?
(ण) ‘आत्मानुभव’ से क्या आशय है ?
(त) ‘माता-पिता’ में कौन-सा समास है ?
उत्तर
(क) गड़रियों का निश्छल जीवन।
(ख) गड़रिये के परिवार में एक बूढ़ा गड़रिया, उसके माता-पिता, उसकी पत्नी, दो बेटियाँ तथा उसकी भेड़ें हैं।
(ग) वह बिना मकान के झोपडी में रहता है।
(घ) लेखक ने अलौकिक खुशी से भरपूर गड़रिये के परिवार को ‘दिव्य परिवार’ कहा है।
(ङ) सौंदर्यमय, अति सुंदर।
(च) आकाश की ओर मुँह उठाकर ईश्वर की आराधना करते हैं।
(छ) बीमार भेड़ के स्वस्थ होने की खुशी में।
(ज) ईश्वरीय आनंद का वातावरण तैयार करना।
(झ) बुड़े, सफेद।
(ञ) पत्नी, नारी।
(ट) युवा अवस्था; कर्मधारय समास।
(ठ) उर्दू – खुदा, फुरसत
तत्सम – शुद्ध, संकल्प
(ड) विद्वान।
(ढ) लेखक अज्ञान के कारण आई आत्य-संतुष्टि को अपनाना चाहता है।
(ण)स्वयं किया गया प्रत्यक्ष अनुभव। यह अनुभव प्रकृति और आत्मा से संबंधित है।
(त) द्वंद्व समास।
10. पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श-पश्चिमी सभ्यता मुख मोड़ रही है। वह एक नया आदर्श देख रही है। अब उसकी चाल बदलने लगी है। वह कलों की पूजा को छोड़कर मनुष्यों की पूजा को अपना आदर्श बना रही है। इस आदर्श के दर्शाने वाले देवता रस्किन और टाल्स्टॉय आदि हैं। पाश्चात्य देशों में नया प्रभात होने वाला है। वहाँ के गंभीर विचार वाले लोग इस प्रभात का स्वागत करने के लिए उठ खड़े हुए हैं। प्रभात होने के पूर्व ही उसका अनुभव कर लेने वाले पक्षियों की तरह इन महात्माओं को इस नए प्रभात का पूर्व ज्ञान हुआ है। और, हो क्यों न? इंजनों के पहिए के नीचे दबकर वहाँ वालों के भाई-बहन-नहीं नहीं उनकी सारी जाति पिस गई; उसके जीवन के धुरे टूट गए, उनका समस्त धन घरों से निकलकर एक ही दो स्थानों में एकत्र हो गया।
साधारण लोग मर रहे हैं, मजदूरों के हाथ-पाँव फट रहे हैं, लहू चल रहा है! सर्दी से ठिठुर रहे हैं। एक तरफ दरिद्रता का अखंड राज्य है, दूसरी तरफ अमीरी का चरम दृश्य। परंतु अमीरी भी मानसिक दुःखों से विमर्दित है। मशीनें बनाई तो गई थी मनुष्यों का पेट भरने के लिए मजदूरों को सुख देने के लिए-परंतु काली-काली मशीनें ही काली बनकर उन्हीं मनुष्यों का भक्षण कर जाने के लिए मुख खोल रही हैं। प्रभात होने पर ये काली-काली बलाएँ दूर होंगी। मनुष्य के सौभाग्य का सूर्योदय होगा।
शोक का विषय है कि हमारे और अन्य पूर्वी देशों में लोगों को मजदूरी से तो लेशमात्र भी प्रेम नहीं, पर वे तैयारी कर रहे हैं पूर्वोक्त काली मशीनों का आलिंगन करने की। पश्चिम वालों के तो ये गले पड़ी हुई बहती नदी की काली कमली हो रही हैं। वे छोड़ना चाहते हैं, परंतु काली कमली उन्हें नहीं छोड़ती। देखेंगे पूर्व वाले इस कमली को छाती से लगाकर कितना आनंद अनुभव करते हैं। यदि हममें से हर आदमी अपनी दस उँगलियों की सहायता से साहसपूर्वक अच्छी तरह काम करे तो हम मशीनों की कृपा से बढ़े हुए परिश्रम वालों को वाणिज्य के जातीय संग्राम में सहज ही पछाड़ सकते हैं। सूर्य तो सदा पूर्व ही से पश्चिम की ओर जाता है। पर, आओ पश्चिम में आने वाली सभ्यता के नए प्रभात को हम पूर्व से भेजें।
इंजनों की वह मजदूरी किस काम की जो बच्चों, स्त्रियों और कारीगरों को ही भूखा-नंगा रखती है, और केवल सोने, चाँदी, लोहे आदि धातुओं का ही पालन करती है। पश्चिम को विदित हो चुका है कि इनसे मनुष्य का दुःख दिन-पर-दिन बढ़ता है। भारतवर्ष जैसे दरिद्र देश में मनुष्य के हाथों की मजदूरी के बदले कलों से काम लेना काल का डंका बजाना होगा। दरिद्र प्रजा और भी दरिद्र होकर मर जाएगी। चेतन से चेतन की वृद्धि होती है। मनुष्य को तो मनुष्य ही सुख दे सकता है। परस्पर को निष्कपट सेवा ही से मनुष्य जाति का कल्याण हो सकता है।
Apathit Gadyansh In Hindi For Class 10 Bihar Board प्रश्न
(क) उचित शीर्षक दीजिए।
(ख)पश्चिमी सभ्यता किससे मुँह मोड़ रही है?
(ग) कलों की पूजा’ का क्या आशय है ?
(घ) मनुष्यों की पूजा’ का क्या अर्थ है ?
(ङ) नया प्रभात’ का संकेतार्थ समझाइए।
(च) पश्चिमी देशों को नए प्रभात का ज्ञान क्यों हुआ है ?
(छ) इंजनों के पहियों के नीचे पिसने का क्या तात्पर्य है ?
(ज)पश्चिमी देशों में धन के कारण कौन-सी बुराई सामने आई ?
(झ) अमीरी मानसिक दुःखों से विमर्दित है”- इसका आशय स्पष्ट कीजिए।
(ञ) चरम दृश्य” का अर्थ स्पष्ट कीजिए।
(ट)लेखक किंसे शोक का विषय मानता है?
(ठ) ‘काली कमली’ किस चीज की प्रतीक है ?
(ड) लेखक भारत में उत्पादन को किस प्रकार बढ़ाने का पक्षधर है?
(ढ) इंजनों की मजदूरी का क्या आशय है ?
(ण) लेखक इंजनों की मजदूरी का विरोधी क्यों है?
(त) ‘काल का डंका बजाना’ का आशय स्पष्ट कीजिए।
(थ) निम्नलिखित वाक्य से नकारात्मक वाक्य बनाइए
परस्पर की निष्कपट सेवा से ही मनुष्य-जाति का कल्याण हो सकता है।
(द) ‘विमर्दित’ में प्रयुक्त उपसर्ग और प्रत्यय अलग कीजिए।
(ध) आलिंगन करने का वाक्य में प्रयोग कीजिए।
(न) गले पड़ी हुई’ का अर्थ स्पष्ट कीजिए।
(प) ‘भूखा-नंगा’ का विग्रह करके समास का नाम लिखिए।
(फ) ‘आनंद-मंगल’ का विग्रह करके समास का नाम लिखिए।
उत्तर-
(क) मजदूरी की महिमा।
(ख) पश्चिमी सभ्यता मशीनीकरण से मुँह मोड़ रही है।
(ग) मशीनों की पूजा, अर्थात् मशीनों को अपनाना।
(घ) मनुष्यों की पूजा का आशय है-मनुष्य के श्रम तथा शक्ति को महत्त्व देना।
(ङ) आध्यात्मिकता का नया युग।
(च) मशीनों और इंजनों के क्रूर शोर तथा उत्पात को देखकर उन्हें नए प्रभात की बात सूझी।
(छ) मशीनीकरण के दुखों से पीड़ित होना।
(ज) पश्चिमी देशों में धन की वृद्धि के कारण अमीर और गरीब की खाई बहुत चौड़ी हो गई। गरीब भूखे तड़पने लगे और अमीर मानसिक दुखों से पागल होने लगे।
(झ) अमीर लोग मानसिक तनावों के कारण बेहद दुखी हैं।
(ञ) सबसे अधिक बढ़ा हुआ दृश्य।
(ट) लेखक भारत द्वारा मशीनीकरण को अपनाने को शोक का विषय मानता है।
(ठ) काली कमली गले में पड़ी हुई दुखदायी वस्तु की प्रतीक है। यहाँ मशीनीकरण काली कमली है।
(ङ) लेखक भारत में मानवीय परिश्रम के सहारे उत्पादन को बढ़ाने का पक्षधर है।
(ढ) मशीनीकरण पर आधारित जीवन-शैली को अपनाना।
(ण) लेखक इंजनों की मजदूरी का विरोधी इसलिए है क्योंकि इससे बेकारी, गरीबी और आर्थिक असमानता बढ़ेगी।
(त) स्वयं मौत को बुलावा देना।
(थ) परस्पर की निष्कपट सेवा से ही मनुष्य-जाति का कल्याण हो सकता है।
(द) उपसर्ग – वि’; प्रत्यय’इत’।
(ध) धोनी ने आखिरी गेंद पर छक्का मारकर विजय-श्री का आलिंगन कर लिया।
(न) जबरदस्ती चिपकी हुई।
(प) भूखा और नंगा; द्वंद्व समासा
(फ) आनंद और मंगल; द्वंद्व समास।
11. शिक्षा को महत्त्वाकांक्षा से मुक्त होना ही चाहिए। महत्त्वाकांक्षा ही तो राजनीति है। महत्त्वाकांक्षा के कारण ही तो राजनीति सबके ऊपर, सिंहासन पर विराजमान हो गई है। सम्मान वहाँ है, जहाँ पद है। पद वहाँ है, जहाँ शक्ति है। शक्ति वहाँ है, जहाँ राज्य है। इस दौड़ से जीवन में हिंसा पैदा होती है। महत्त्वाकांक्षी चित्त हिंसक चित्त है। अहिंसा के पाठ पढ़ाए जाते हैं। साथ ही महत्त्वाकांक्षा भी सिखाई जाती है। इससे ज्यादा मूढ़ता और क्या हो
सकती है?
अहिंसा प्रेम है। महत्त्वाकांक्षा प्रतिस्पर्धा है। प्रेम सदा पीछे रहना चाहता है। प्रतिस्पर्धा आगे होना चाहती है। क्राइस्ट ने कहा है-‘धन्य हैं वे, जो पीछे होने में समर्थ हैं।’ मैं जिसे प्रेम करूँगा, उसे आगे देखना चाहूँगा और यदि मैं सभी को प्रेम करूंगा तो स्वयं को सबसे पीछे खड़ाकर आनंदित हो उलूंगा। लेकिन प्रतिस्पर्धा प्रेम से बिल्कुल उलटी है। वह तो ईर्ष्या है। वह तो घृणा है। वह तो हिंसा है। वह तो सब भाँति सबसे आगे होना चाहती है।
इस आगे होने की होड़ की शुरूआत शिक्षालयों में ही होती है और फिर कब्रिस्तान तक चलती है। व्यक्तियों में यही दौड़ है। राष्ट्रों में भी यही दौड़ है। युद्ध इस दौड़ के ही तो अंतिम फल हैं। यह दौड़ क्यों है ? इस दौड़ के मूल में क्या है ? मूल में है—-अहंकार! हंकार सिखाया जाता है, अहंकार का पोषण किया जाता है।
छोटे-छोटे बच्चों में अहंकार को जगाया और जलाया जाता है। उनके निर्दोष और सरल चित्त अहंकार से विषाक्त किए जाते हैं। उन्हें भी प्रथम होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। स्वर्ण पदक और सम्मान और पुरस्कार बाँटे जाते हैं। फिर यही अहंकार जीवन-भर प्रेत की भाँति उनका पीछा करता है और उन्हें मरते दम तक चैन नहीं लेने देता। विनय के उपदेश दिए जाते हैं और सिखाया अहंकार जाता है। क्या वह दिन मनुष्य जाति के इतिहास में सबसे बड़े सौभाग्य का दिन नहीं होगा जिस दिन हम बच्चों को अहंकार सिखाना बंद कर देंगे? अहंकार नहीं, प्रेम सिखाना है। और प्रेम वहीं होता है, जहाँ अहंकार नहीं है।
‘इसके लिए शिक्षण की आमूल पद्धति ही बदलनी होगी। प्रथम और अंतिम की कोटियाँ तोड़नी होंगी। परीक्षाओं को समाप्त करना होगा। और इन सबकी जगह जीवन के उन मूल्यों की स्थापना करनी होगी जो कि अहंशून्य और प्रेमपूर्ण जीवन को सर्वोच्च जीवन-दर्शन मानने से पैदा होते हैं।
प्रश्न-
(क) इस गद्यांश का शीर्षक दीजिए।
(ख) लेखक महत्त्वाकांक्षा की जगह कैसी शिक्षा चाहता है ?
(ग) महत्त्वाकांक्षा को राजनीति कहने का क्या आशय है ?
(घ) प्रेमी की पहचान क्या है ?
(ङ) प्रतिस्पर्धा से कौन-से दुर्गुण पैदा होते हैं ?
(च) लेखक बच्चों को प्रतियोगिता क्यों नहीं सिखाना चाहता?
(छ) लेखक स्वर्ण-पदक और सम्मान का विरोध क्यों करता है ?
(ज) लेखक शिक्षा में किस प्रकार का परिवर्तन चाहता है ?
(झ) दो उर्दू तथा तत्सम शब्द छाँटिए।
(ञ) दो ऐसे वाक्य छाँटिए, जिसमें निपात का प्रयोग हो।
(ट) एक सरल, संयुक्त तथा मिश्र वाक्य छाँटिए।
(ठ) निर्दोष, सरल, अहंकार, समर्थ, हिंसक के विलोम लिखिए।
(ड) महत्त्वाकांक्षी, मूढ़, हिंसक, सफलता, आनंदित से भाववाचक संज्ञाएँ बनाइए।
उत्तर-
(क) स्पर्धा-मुक्त शिक्षा की आवश्यकता।
(ख) लेखक महत्त्वाकांक्षा की जगह अहंशून्यता और प्रेम की शिक्षा देना चाहता है।
(ग) महत्त्वाकांक्षा को पूरा करने वाला आदमी शक्ति चाहता है। शक्ति राजनीति में है। इसलिए महत्त्वाकांक्षा का दूसरा नाम ही राजनीति है।
(घ) प्रेमी व्यक्ति की पहचान है कि वह सदा अपने प्रियजनों को अपने से आगे रखना चाहता है और स्वयं पीछे रहना चाहता है।
(ङ) प्रतिस्पर्धा से आपसी ईर्ष्या पैदा होती है, घृणा पैदा होती हे और हिंसा पैदा होती है।
(च) लेखक बच्चों को प्रतिस्पर्धा में नहीं डालना चाहता। कारण यह है कि इससे बच्चों में अहंकार पैदा होता है। वे ईर्ष्या, घृणा ओर हिंसा करना सीखते हैं।
(छ) लेखक के अनुसार स्वर्ण-पदक और सम्मान मनुष्य के अहंकार को बढ़ाते हैं। इन्हें पाकर मनुष्य स्वयं को विशिष्ट, ऊँचा और महत्त्वपूर्ण मानने लगता है। इससे उसके जीवन में प्रेम नहीं आ पाता।
(ज) लेखक चाहता है कि वर्तमान शिक्षा-प्रणाली में से अहंकार जगाने वाली बातें समाप्त करनी चाहिए। प्रथम आने की भावना, स्वर्ण पदक पाने की होड़, सम्मान पाने की आकांक्षा, परीक्षा-प्रणाली में प्रथम या अंतिम रह जाने की भावनाएँ—मन को अस्वस्थ बनाती हैं। इन्हें समाप्त करना चाहिए। इनकी बजाय प्रेम और सहयोग पैदा करने की प्रणाली अपनानी चाहिए।
(झ) उर्दू – ज्या, कब्रिस्तान
तत्सम – महत्त्वाकांक्षा, चित्त।
(ञ) 1. राष्ट्रों में भी यही दौड़ है।
2. सफलता ही जहाँ एकमात्र मूल्य है, वहाँ सत्य नहीं हो सकता।
(ट) सरल – अहिंसा प्रेम है।
संयुक्त – आगे होने की दौड़ शिक्षालयों में ही शुरू होती है और फिर कब्रिस्तान तक चलती है।
मिश्र – सम्मान वहाँ है, जहाँ पद है।
(ठ) निर्दोष – सदोष, दोषी
सरल – जटिला
अहंकार – प्रेमा
समर्थ – असमर्थ।
हिंसक – अहिंसक।
(ड) महत्त्वाकांक्षी – महत्त्वाकांक्षा।
मूढ़ – मूढ़ता।
हिंसक – हिंसा।
सफल – सफलता।
आनंदित – आनंद।
BSEB Textbook Solutions PDF for Class 10th
- BSEB Class 10 Textbook Solutions PDF: Download Bihar Board STD 10th Book Answers
- BSEB Class 10 Hindi Textbook Solutions PDF: Download Bihar Board STD 10th Hindi Book Answers
- BSEB Class 10 Hindi Godhuli Chapter 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा Textbook Solutions PDF: Download Bihar Board STD 10th Hindi Godhuli Chapter 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा Book Answers
- BSEB Class 10 Hindi Godhuli Chapter 2 विष के दाँत Textbook Solutions PDF: Download Bihar Board STD 10th Hindi Godhuli Chapter 2 विष के दाँत Book Answers
- BSEB Class 10 Hindi Godhuli Chapter 3 भारत से हम क्या सीखें Textbook Solutions PDF: Download Bihar Board STD 10th Hindi Godhuli Chapter 3 भारत से हम क्या सीखें Book Answers
- BSEB Class 10 Hindi Godhuli Chapter 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं Textbook Solutions PDF: Download Bihar Board STD 10th Hindi Godhuli Chapter 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं Book Answers
- BSEB Class 10 Hindi Godhuli Chapter 5 नागरी लिपि Textbook Solutions PDF: Download Bihar Board STD 10th Hindi Godhuli Chapter 5 नागरी लिपि Book Answers
- BSEB Class 10 Hindi Godhuli Chapter 6 बहादुर Textbook Solutions PDF: Download Bihar Board STD 10th Hindi Godhuli Chapter 6 बहादुर Book Answers
- BSEB Class 10 Hindi Godhuli Chapter 7 परंपरा का मूल्यांकन Textbook Solutions PDF: Download Bihar Board STD 10th Hindi Godhuli Chapter 7 परंपरा का मूल्यांकन Book Answers
- BSEB Class 10 Hindi Godhuli Chapter 8 जित-जित मैं निरखत हूँ Textbook Solutions PDF: Download Bihar Board STD 10th Hindi Godhuli Chapter 8 जित-जित मैं निरखत हूँ Book Answers
- BSEB Class 10 Hindi Godhuli Chapter 9 आविन्यों Textbook Solutions PDF: Download Bihar Board STD 10th Hindi Godhuli Chapter 9 आविन्यों Book Answers
- BSEB Class 10 Hindi Godhuli Chapter 10 मछली Textbook Solutions PDF: Download Bihar Board STD 10th Hindi Godhuli Chapter 10 मछली Book Answers
- BSEB Class 10 Hindi Godhuli Chapter 11 नौबतखाने में इबादत Textbook Solutions PDF: Download Bihar Board STD 10th Hindi Godhuli Chapter 11 नौबतखाने में इबादत Book Answers
- BSEB Class 10 Hindi Godhuli Chapter 12 शिक्षा और संस्कृति Textbook Solutions PDF: Download Bihar Board STD 10th Hindi Godhuli Chapter 12 शिक्षा और संस्कृति Book Answers
- BSEB Class 10 Hindi Godhuli Chapter 1 राम बिनु बिरथे जगि जनमा, जो नर दुख में दुख नहिं मानै Textbook Solutions PDF: Download Bihar Board STD 10th Hindi Godhuli Chapter 1 राम बिनु बिरथे जगि जनमा, जो नर दुख में दुख नहिं मानै Book Answers
- BSEB Class 10 Hindi Godhuli Chapter 2 प्रेम अयनि श्री राधिका, करील के कुंजन ऊपर वारौं Textbook Solutions PDF: Download Bihar Board STD 10th Hindi Godhuli Chapter 2 प्रेम अयनि श्री राधिका, करील के कुंजन ऊपर वारौं Book Answers
- BSEB Class 10 Hindi Godhuli Chapter 3 अति सूधो सनेह को मारग है, मो अंसुवानिहिं लै बरसौ Textbook Solutions PDF: Download Bihar Board STD 10th Hindi Godhuli Chapter 3 अति सूधो सनेह को मारग है, मो अंसुवानिहिं लै बरसौ Book Answers
- BSEB Class 10 Hindi Godhuli Chapter 4 स्वदेशी Textbook Solutions PDF: Download Bihar Board STD 10th Hindi Godhuli Chapter 4 स्वदेशी Book Answers
- BSEB Class 10 Hindi Godhuli Chapter 5 भारतमाता Textbook Solutions PDF: Download Bihar Board STD 10th Hindi Godhuli Chapter 5 भारतमाता Book Answers
- BSEB Class 10 Hindi Godhuli Chapter 6 जनतंत्र का जन्म Textbook Solutions PDF: Download Bihar Board STD 10th Hindi Godhuli Chapter 6 जनतंत्र का जन्म Book Answers
- BSEB Class 10 Hindi Godhuli Chapter 7 हिरोशिमा Textbook Solutions PDF: Download Bihar Board STD 10th Hindi Godhuli Chapter 7 हिरोशिमा Book Answers
- BSEB Class 10 Hindi Godhuli Chapter 8 एक वृक्ष की हत्या Textbook Solutions PDF: Download Bihar Board STD 10th Hindi Godhuli Chapter 8 एक वृक्ष की हत्या Book Answers
- BSEB Class 10 Hindi Godhuli Chapter 9 हमारी नींद Textbook Solutions PDF: Download Bihar Board STD 10th Hindi Godhuli Chapter 9 हमारी नींद Book Answers
- BSEB Class 10 Hindi Godhuli Chapter 10 अक्षर-ज्ञान Textbook Solutions PDF: Download Bihar Board STD 10th Hindi Godhuli Chapter 10 अक्षर-ज्ञान Book Answers
- BSEB Class 10 Hindi Godhuli Chapter 11 लौटकर आऊँग फिर Textbook Solutions PDF: Download Bihar Board STD 10th Hindi Godhuli Chapter 11 लौटकर आऊँग फिर Book Answers
- BSEB Class 10 Hindi Godhuli Chapter 12 मेरे बिना तुम प्रभु Textbook Solutions PDF: Download Bihar Board STD 10th Hindi Godhuli Chapter 12 मेरे बिना तुम प्रभु Book Answers
- BSEB Class 10 Hindi Varnika Chapter 1 दही वाली मंगम्मा Textbook Solutions PDF: Download Bihar Board STD 10th Hindi Varnika Chapter 1 दही वाली मंगम्मा Book Answers
- BSEB Class 10 Hindi Varnika Chapter 2 ढहते विश्वास Textbook Solutions PDF: Download Bihar Board STD 10th Hindi Varnika Chapter 2 ढहते विश्वास Book Answers
- BSEB Class 10 Hindi Varnika Chapter 3 माँ Textbook Solutions PDF: Download Bihar Board STD 10th Hindi Varnika Chapter 3 माँ Book Answers
- BSEB Class 10 Hindi Varnika Chapter 4 नगर Textbook Solutions PDF: Download Bihar Board STD 10th Hindi Varnika Chapter 4 नगर Book Answers
- BSEB Class 10 Hindi Varnika Chapter 5 धरती कब तक घूमेगी Textbook Solutions PDF: Download Bihar Board STD 10th Hindi Varnika Chapter 5 धरती कब तक घूमेगी Book Answers
- BSEB Class 10 Hindi व्याकरण अपठित गद्यांश Textbook Solutions PDF: Download Bihar Board STD 10th Hindi व्याकरण अपठित गद्यांश Book Answers
- BSEB Class 10 Hindi व्याकरण पत्र लेखन Textbook Solutions PDF: Download Bihar Board STD 10th Hindi व्याकरण पत्र लेखन Book Answers
- BSEB Class 10 Hindi व्याकरण निबंध लेखन Textbook Solutions PDF: Download Bihar Board STD 10th Hindi व्याकरण निबंध लेखन Book Answers
- BSEB Class 10 Hindi व्याकरण संज्ञा Textbook Solutions PDF: Download Bihar Board STD 10th Hindi व्याकरण संज्ञा Book Answers
- BSEB Class 10 Hindi व्याकरण सर्वनाम Textbook Solutions PDF: Download Bihar Board STD 10th Hindi व्याकरण सर्वनाम Book Answers
- BSEB Class 10 Hindi व्याकरण लिंग Textbook Solutions PDF: Download Bihar Board STD 10th Hindi व्याकरण लिंग Book Answers
- BSEB Class 10 Hindi व्याकरण वाक्य प्रयोग द्वारा लिंग निर्णय Textbook Solutions PDF: Download Bihar Board STD 10th Hindi व्याकरण वाक्य प्रयोग द्वारा लिंग निर्णय Book Answers
- BSEB Class 10 Hindi व्याकरण क्रिया-भेद Textbook Solutions PDF: Download Bihar Board STD 10th Hindi व्याकरण क्रिया-भेद Book Answers
- BSEB Class 10 Hindi व्याकरण विशेषण और क्रिया विशेषण Textbook Solutions PDF: Download Bihar Board STD 10th Hindi व्याकरण विशेषण और क्रिया विशेषण Book Answers
- BSEB Class 10 Hindi व्याकरण पद परिचय Textbook Solutions PDF: Download Bihar Board STD 10th Hindi व्याकरण पद परिचय Book Answers
- BSEB Class 10 Hindi व्याकरण वाक्य-भेद Textbook Solutions PDF: Download Bihar Board STD 10th Hindi व्याकरण वाक्य-भेद Book Answers
- BSEB Class 10 Hindi व्याकरण मुहावरे और लोकोक्तियाँ Textbook Solutions PDF: Download Bihar Board STD 10th Hindi व्याकरण मुहावरे और लोकोक्तियाँ Book Answers
- BSEB Class 10 Hindi व्याकरण अलंकार Textbook Solutions PDF: Download Bihar Board STD 10th Hindi व्याकरण अलंकार Book Answers






0 Comments:
Post a Comment