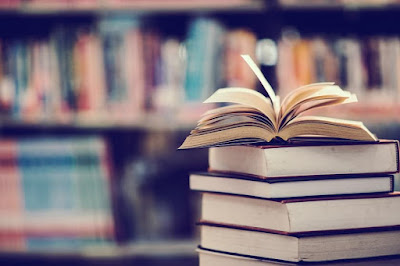 |
| BSEB Class 8 Hindi व्याकरण Textbook Solutions PDF: Download Bihar Board STD 8th Hindi व्याकरण Book Answers |
Bihar Board Class 8th Hindi व्याकरण Textbooks Solutions PDF
Bihar Board STD 8th Hindi व्याकरण Books Solutions with Answers are prepared and published by the Bihar Board Publishers. It is an autonomous organization to advise and assist qualitative improvements in school education. If you are in search of BSEB Class 8th Hindi व्याकरण Books Answers Solutions, then you are in the right place. Here is a complete hub of Bihar Board Class 8th Hindi व्याकरण solutions that are available here for free PDF downloads to help students for their adequate preparation. You can find all the subjects of Bihar Board STD 8th Hindi व्याकरण Textbooks. These Bihar Board Class 8th Hindi व्याकरण Textbooks Solutions English PDF will be helpful for effective education, and a maximum number of questions in exams are chosen from Bihar Board.Bihar Board Class 8th Hindi व्याकरण Books Solutions
| Board | BSEB |
| Materials | Textbook Solutions/Guide |
| Format | DOC/PDF |
| Class | 8th |
| Subject | Hindi व्याकरण |
| Chapters | All |
| Provider | Hsslive |
How to download Bihar Board Class 8th Hindi व्याकरण Textbook Solutions Answers PDF Online?
- Visit our website - Hsslive
- Click on the Bihar Board Class 8th Hindi व्याकरण Answers.
- Look for your Bihar Board STD 8th Hindi व्याकरण Textbooks PDF.
- Now download or read the Bihar Board Class 8th Hindi व्याकरण Textbook Solutions for PDF Free.
BSEB Class 8th Hindi व्याकरण Textbooks Solutions with Answer PDF Download
Find below the list of all BSEB Class 8th Hindi व्याकरण Textbook Solutions for PDF’s for you to download and prepare for the upcoming exams:BSEB Bihar Board Class 8 Hindi व्याकरण Grammar
वर्गों के उच्चारण स्थान
उच्चारण-स्थान – वर्ण
- कंठ – अ, आ, क, ख, ग, घ, ह तथा विसर्ग (:)
- तालु – इ, ई, च, छ, ज, झ, य तथा श
- मूर्द्धा – ऋ, ट, ठ, ड, ढ, र, प . दंत
- दंत – त, थ, द, ध, न, ल और स
- ओष्ठ – उ, ऊ, प, फ, ब, भ
- कंठ और नारिका – ड.
- तालु और नासिका – ब
- मूर्द्धा और नासिका – ण
- ओष्ठ और नासिका – म
- कंठ और तालु – ए और ऐ (दीर्घ स्वर, द्विमात्रिक स्वर एवं संयुक्त स्वर)
- कंठ और ओष्ठ – ओ और औ (दीर्घ स्वर, द्विमात्रिक स्वर एवं संयुक्त स्वर)
- दंत और ओष्ठ – व
- अघोष वर्ण – क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, प, स,
- (प्रत्येक वर्ग के प्रथम दो वर्ण तथा श.प.स)
- घोष वर्ण – ग, घ, ज, झ, ड, ढ, द, ध, ब, भ, ङ, ञ, ण, न, य, र, ल, व, ह, म, अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ (प्रत्येक वर्ग के अंतिम
- तीनों वर्ण तथा य, र, ल, व, ह एवं सभी स्वर वर्ण ।)
- अल्पप्राण – क, ग, ङ, च, ज, ब, ट, ड, ण, त, द, न, प, ब,म
- महाप्राण – ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, फ, भ, थ, ध
- ऊष्ण वर्ण – श, ष, स, ह,
- अंत:स्थ – य, र, ल, व, अ, इ, उ तथा ऋ को ह्रस्व/एकमात्रिक
- और मूल स्वर कहा जाता है । क्ष (क् + ष), त्र (त् + र) और ज्ञ (ज् + ज् ) संयुक्त वर्ण हैं।
शब्द
प्रश्न 1.
शब्द किसे कहते हैं ?
उत्तर:
ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण-समुदाय को ‘शब्द’ कहते हैं।
प्रश्न 2.
‘अर्थ’ के अनुसार शब्दों के कितने भेद हैं ?
उत्तर:
अर्थ के अनुसार शब्दों के दो भेद हैं
- सार्थक-जिन शब्दों का स्वयं कुछ अर्थ होता है, उसे सार्थक शब्द कहते हैं । जैसे-घर, लड़का, चित्र आदि ।
- निरर्थक-जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, उसे निरर्थक शब्द कहते हैं । जैसे-चप, लव, कट आदि
प्रश्न 3.
व्युत्पत्ति के अनुसार शब्दों के कौन-कौन से भेद हैं ?
उत्तर:
व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के चार भेद हैं ।
- तत्सम – संस्कृत के सीधे आए शब्दों को तत्सम कहते हैं । जैसे- रिक्त, जगत्, मध्य, छात्र ।
- तद्भव – संस्कृत से रूपान्तरित होकर हिन्दी में आए शब्दों को तद्भव कहते हैं। जैसे-आग, हाथ, खेत आदि ।
- देशज – देश के अन्दर बोल-चाल के कुछ शब्द हिन्दी में आ गए हैं । इन्हें देशज कहा जाता है जैसे- लोटा, पगडी, चिडिया, पेट आदि ।
- विदेशज – कुछ विदेशी भाषा के शब्द हिन्दी में मिला लिये गए हैं, इन्हें विदेशज शब्द कहते हैं । जैसे-स्कूल, कुर्सी, तकिया, टेबुल, मशीन, बटन, किताब, बाग आदि ।
प्रश्न 4.
उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं ?
उत्तर:
उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के तीन भेद हैं।
- रूढ़-जिन शब्दों के खंड़ों का अलग-अलग अर्थ नहीं होता, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं । जैसे-जल = ज + ल ।
- यौगिक-जिन शब्दों के अलग-अलग खंडों का कुछ अर्थ हो, उसे यौगिक शब्द कहते हैं । जैसे-हिमालय, पाठशाला, देवदूत, विद्यालय आदि ।
- योगरूढ़-जो शब्द सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बतावे, उसे योगरूढ़ कहते हैं । जैसे-लम्बोदर (गणेश), चक्रपाणि (विष्णु) चन्द्रशेखर (शिवजी) आदि ।
संज्ञा
प्रश्न 1.
संज्ञा किसे कहते हैं ?
उत्तर:
किसी प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव को संज्ञा कहते हैं।
प्रश्न 2.
संज्ञा के कितने भेद हैं ? वर्णन करें।
उत्तर:
संज्ञा के निम्नांकित पाँच भेद हैं।
- व्यक्तिवाचक संज्ञा-किसी विशेष प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम -को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे-राम, श्याम, हिमालय, पटना, पूर्णिया आदि ।
- जातिवाचक संज्ञा-जिस संज्ञा से किसी जाति के सभी पदार्थों का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं । जैसे- गाय, घोड़ा, फूल, आदमी औरत आदि ।
- भाववाचक संज्ञा-जिस से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण-धर्म और स्वभाव का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं । जैसे-बुढ़ापा, चतुराई, मिठास आदि ।
- समूहवाचक संज्ञा-जिस शब्द से समूह या झुण्ड का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं । जैसे-सोना, वर्ग, भीड़, सभा आदि ।
- द्रव्यवाचक संज्ञा-जिन वस्तुओं को नापा-तौला जा सके, ऐसी वस्तु के नामों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं । जैसे-तेल, घी, पानी, सोना आदि ।
भाववाचक संज्ञा बनाना
(i) जातिवाचक संज्ञा से

(ii) सर्वनाम से

(iii) विशेषण से

(iv) क्रिया से

संधि
प्रश्न 1.
संधि किस कहते हैं ?
उत्तर:
जब दो या दो से अधिक वर्ण मिलते हैं, तो इससे पैदा होने वाला विकार को संधि कहते हैं । जैसे – जगत् + नाथ = जगन्नाथ, शिव + आलय = शिवालय, गिरि + ईश = गिरीश आदि ।
प्रश्न 2.
संधि के कितने भेद हैं ?
उत्तर:
संधि के तीन भेद हैं-
- स्वर संधि
- व्यंजन संधि
- विसर्ग संधि ।
प्रश्न 3.
स्वर संधि किसे कहते हैं ?
उत्तर:
दो या दो से अधिक स्वर वर्णों के मिलने से जो विकार पैदा होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे – अन्न + अभाव = अन्नाभाव, महा + आशय = महाश्य, भोजन + आलय = भोजनालय ।
प्रश्न 4.
स्वर संधि के कितने भेद हैं ? उनके विषय में लिखें ।
उत्तर:
स्वर संधि के पाँच भेद हैं :
- दीर्घ संधि-जब ह्रस्व या दीर्घ वर्ण, ह्रस्व या दीर्घ वर्णों से मिलकर दीर्घ स्वर हो जाते हैं, उसे दीर्घ संधि कहते हैं । जैसे भोजन + आलय = भोजनालाय (अ + आ = आ) अन्न + अभाव = अन्नाभाव (अ + आ = आ) गिरि + इन्द्र = गिरीन्द्र (इ + ई = ई) विधु + उदय = विधूदय (उ + उ = ऊ) .
- गुण संधि-यदि ‘अ’ या ‘आ’ के बाद इ, ई, उ, ऊ, ऋ आवे तो वे मिलकर क्रमशः ए, ओ और अर् हो जाते हैं । जैसे – नर + इन्द्र = नरेन्द्र, देव + ईश = देवेश, महा + ऋषि = महर्षि आदि ।
- वृद्धि संधि-यदि ह्रस्व या दीर्घ ‘अ आ’ के बाद ए, ऐ आवे तो – ‘ऐ’ और ‘ओ’ आवे तो ‘औ’ हो जाते हैं । जैसे-अनु + एकान्त = अनैकान्त, तथा + एव = तथैव, वन + औषधि = वनौषधि, सुन्दर + ओदन = सुन्दरौदन ।
- यण संधि-इ, ई के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो ‘य’, उ, ऊ, के बाद भिन्न स्वर आवे तो ‘व्’ और ऋ के बाद भिन्न स्वर आवे तो ‘र’ हो · जाता है.। जैसे-सखी + उवाच = सख्युवाच, दधि + आयन = दध्यानय, अनु + अय = अन्वय, अनु + एषण = अन्वेषण, पित + आदेश = पित्रादेश ।
- अयादि संधि-यदि ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भिन्न स्वर हो, तो उसके स्थान पर क्रमशः ‘अय्’, ‘आय’, ‘आव्’ हो जाता है । जैसे-ने + अन = नयन । गै अक = गायक, भो + अन = भवन, भौ + उक = भावुक
प्रश्न 5.
व्यंजन संधि किसे कहते हैं ?
उत्तर:
व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन या स्वर वर्ण के मिलने से जो विकार पैदा होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं । जैसे-दिक् + अन्त = दिगन्त, दिक् + गज = दिग्गज, जगत् + ईश = जगदीश, जगत् + नाथ = जगन्नाथ, सत् + आनन्द = सदानन्द, उत् + घाटन = उद्घाटन ।।
प्रश्न 6.
विसर्ग संधि किसे कहते हैं ? सोदाहरण परिभाषा दें।
उत्तर:
विसर्ग (:) के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से जो विकार पैदा होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं । जैसे-निः + चय – निश्चय, निः + पाप = निष्पाप ।
स्मरणीय
- अप् + ज = अब्ज
- उत् + गम = उद्गम
- अनि + आय = अन्याय
- उपरि + उक्त = उपर्युक्त
- पृष् + थ = पृष्ठ
- सम् + सार = संसार
- अन्तः + पुर = अन्तःपुर
- उत् + लेख = उल्लेख
- अति + अधिक = अत्यधिक
- तपः + वन = तपोवन
- आशी: + वाद = आशीर्वाद
- वि + आकुल = व्याकुल
- आ + छादन = आच्छादन
- वयः + वृद्ध = वयोवृद्ध
- आदि + अन्त = आद्यन्त
- राज + ऋषि = राजर्षि
- अभि + इष्ट = अभीष्ट
- पो +’ इत्र = पवित्र
- राम + अयन = रामायण
- पुरः + कार = पुरस्कार
- दिक् + भ्रम = दिग्भ्रम
- परि + ईक्षा = परीक्षा
- देव + ऋषि = देवर्षि
- पीत + अम्बर = पीताम्बर
- नमः + कार = नमस्कार
- पयः + धिं = पयोधि ।
- नार + अयन = नारायण
- परम् + तु = परन्तु
- नारी + ईश्वर = नारीश्वर
- परम + ईश्वर = परमेश्वर
- नौ+ इक = नाविक
- प्रति + एक . = प्रत्येक
- ने+ अन = नयन
- निः + रोग = नीरोग
- शिर: + मणि = शिरोमणि
- भानु + उदय = भानूदय
- उत् + लंघन = उल्लंघन
- सु + आगत = स्वागत
लिंग
प्रश्न 1
लिंग किसे कहा जाता है ?
उत्तर:
संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया के जिस रूप से व्यक्ति, वस्तु और भाव की जाति का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं । हिन्दी शब्द में संज्ञा-शब्द मूल रूप से दो जातियों के हुआ करते हैं- पुरुष-जाति और स्त्री-जाति ।
प्रश्न 2.
लिंग के कितने भेद हैं ? वर्णन करें।
उत्तर:
लिंग के दो भेद हैं
- पँल्लिग-जिस संज्ञा शब्द से पुरुष-जाति का बोध होता है. उसे पुंल्लिग कहते हैं । जैसे-घोड़ा, बैल, लड़का, छात्र, आदि ।
- स्त्रीलिंग-जिस संज्ञा शब्द से ‘स्त्री-जाति’ का बोध होता है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं । जैसे-स्त्री, घोड़ी, गाय, लकड़ी, छात्रा, आदि। जिन प्राणिवाचक शब्दों के जोड़े होते हैं, उनके लिंग आसानी से जाने जा सकते हैं । जैसे- लड़का-लड़की, पुरुष-स्त्री, घोड़ा-घोड़ी, कुत्ता-कुढ़िया ।
गरुड़, बाज, चीता और मच्छर आदि ऐसे शब्द हैं, जो सदा पुंल्लिग होते हैं। मक्खी, मैना, मछली आदि शब्द सदा स्त्रीलिंग होते हैं।
वाक्य प्रयोग द्वारा लिंग निर्णय
- कसक (स्त्री.) – उसके दिल में एक कसक छुपी थी।
- उपेक्षा (स्त्री.) – हर बात की उपेक्षा ठीक नहीं होती ।
- एकांकी (पृ.) – कल क्लब में एकांकी (नाटक) खेला गया ।
- चुनाव (पुं.) – चौदहवां आम चुनाव सम्पन्न हुआ।
- चोंच (स्त्री.) – कौआ की चोंच टूट गई।
- आँख (स्त्री.) – उसकी आँखों में लगा काजल धूल गया ।
- ओस (स्त्री.) – रात भर ओस गिरती रही।
- ईंट (स्त्री.) – नींव की ईंट हिल गई।
- किरण (स्त्री.) – सुनहली किरण छा गई है।
- खबर (स्त्री.) – आज की नई खबर क्या है?
- अनाज (पुं.) – आजकल अनाज महँगा है।
- आयात (पुं.) – हमारे देश का आयात अब संतुलित है।
- आकाश (पृ.) – आकाश नीला था।
- गान (पु.) – उसके बाद एक मधुर गान हुआ ।
- घास (स्त्री.) – यहाँ की घास मुलायम है।
- घूस (स्त्री.) – दारोगा ने घूस ली थी।
- कोदो (पुं.) – खेत में कोदो तैयार थे।
- कोशिश (स्त्री.) – हमारी कोशिश जारी है।
- गरदन (स्त्री.) – उसकी गरदन लम्बी है।
- कौंसिल (स्त्री.) – विचार करने के लिए कौंसिल बैठी ।
- जमानत (स्त्री.) – मोहन की जमानत मंजूर हो गई ।
- जहाज (पं.) – जहाज चला जा रहा था।
- जीत (स्त्री.) – चुनाव में विरोधियों की जीत हुई।
- जेब (स्त्री.) – किसी ने मेरी जेब काट ली ।
- दफ्तर (पुं.) – दफ्तर दस बजे के बाद खुलता है।
- कौंसिल (स्त्री.)-विचार करने के लिए कौंसिल बैठी ।
- जहाज (पुं.)-जहाज चला जा रहा था।
- जीत (स्त्री.)-चुनाव में विरोधियों की जीत हुई।
- जेब (स्त्री.)-किसी ने मेरी जेब काट ली।
- दफ्तर (पुं.)-दफ्तर दस बजे के बाद खुलता है।
- दर्शन (पुं.)-बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन हुए।
- दलदल (स्त्री.)-इस ओर गहरी दलदल थी।
- तनखाह (स्त्री.)-आपकी तनखाह कितनी है ?
- टीस (स्त्री.) – कलेजे में एक टीस-सी उठी।
- जेल (पृ.)-बेउर जेल बहुत बड़ा है।
- जोश (पुं.)-अब उनका जोश ठंडा हो गया था।
- झील (स्त्री.)-आगे दूर तक नीली झील फैली थी।
- ठोकर (स्त्री.)-उसे कसकर ठोकर लगी।
- तलवार (स्त्री.)-वीर की तलवार चमक उठी।
- तलाश (पु.)-सुख की तलाश में सभी लगे हैं।
- “तेल (पुं.)-चमेली का तेल ठंढा होता है।
- तिल (पुं.)-अच्छा तिल बाजार में नहीं बिकता।
- तीतर (पुं.)-आहट पाकर तीतर उड़ गया।
- डाक (स्त्री.)-सुबह की डाक में कोई चिट्ठी नहीं थी।
- ढाढ़स (पुं.)-इस बार ढाढ़स जाता रहा ।
- तान (स्त्री.)-थोड़ी देर बाद एक सुरीली तान सुनाई पड़ी।
- ताबीज (पु.)-फकीर ने अपना ताबीज मुझे दिया ।
- ढेर (पृ.)-वहाँ फूलों का ढेर लगा था ।
- तकदीर (स्त्री.)-उसकी तकदीर ही खोटी है।
- थकान (स्त्री.)-चलने से काफी थकान हो गई थी।
- दाल (स्त्री.)-इस बार उसकी दाल नहीं गली ।
- तह (स्त्री.)-कपड़े की तह खराब न हो ।
- तीर (पुं.)-नावक के तीर छोटे, पर पैने होते हैं।
- दीप (पु.) – दीप जगमगा उठा।
- दीवार (स्त्री.) – दीवारें ढह गई थीं।
- हींग (स्त्री.) – नेपाली हींग अच्छी होती है।
- धोखा (पुं.)-जीवन में हर किसी को धोखा होता है ।
- नमक (पु.) – नमक जल्द गल जाता है।
- नल (पृ.) – वह नल सुबह से ही खुला हुआ था ।
- नसीहत (स्त्री.)-मैंने उसकी नसीहत का कभी बुरा नहीं माना ।
- द्वीप (पुं.)-समुद्र में वह द्वीप अकेला सा है ।
- दूब (स्त्री.)-हरी भरी दूब प्यारी लगती है।
- देवता (पं.)-साहित्य के देवता आजकल मौन हैं।
- देह (स्त्री.)-उसकी देह कमजोर है।
- धुन (स्त्री.)-उन्हें हमेशा कुछ करने की धुन लगी रहती है ।
- नाखून (स्त्री.)-उसके नाखून बढ़े हुए हैं।
- निराशा (स्त्री.) – इस बात से उन्हें गहरी निराशा हुई।
- नोंद (स्त्री.) – उसे नींद आ गई थी।
- पंछी (पुं.) – पंछी आसमान में उड़ रहा था ।
- नीलम (स्त्री:) – रास्ते की धूल में नीलम पड़ा था ।
- नेत्र (पु.) – विषाद से उसके नेत्र बन्द थे।
- पताका (स्त्री.) – उनके यश की पताका विदेशों में फहराने लगी।
- परछाई (स्त्री.) – सुबह में किसी की परछाई कितनी लंबी दीखती है।
- पानी (प.) – बाढ़ का पानी अब तेजी से उतर रहा है।
- पीतल (पृ.) – यह पीतल काफी चमक रहा है।
- पुकार (स्त्री.) – न्याय की पुकार आज कोई नहीं सुनता ।
- पुड़िया (स्त्री.) – बाबाजी ने जादू की पुड़िया खोली।
- पराकाष्ठा (स्त्री.) – उदारता की पराकाष्ठा दानवीर कर्ण में मिलती है।
- परीक्षा (स्त्री.) – जीवन में सभी की परीक्षा होती है।
- पलीता (पुं.) – किले की नींव में पलीता लगा दिया गया ।
- पहचान (स्त्री.) – गुणी व्यक्ति की पहचान में मुझसे भूल नहीं हो सकती।
- मोती (पुं.) – उसकी चूड़ियों में मोती जड़े थे।
- वेतम (स्त्री) – कर्मचारियों का वेतन बढ़ना चाहिए।
- शपथ (स्त्री.) – उसने देश की मान रक्षा की शपथ ली।
- शहद (पु.) – शहद बडा मीठा है।
- पुष्प (पुं.) – उस वृंत पर ही पुष्प खिला था ।
- पुस्तकालय (पुं.) – उस गाँव में एक भी पुस्तकालय नहीं था । ।
- पूर्णिमा (स्त्री.) – कार्तिक की रजताभ पूर्णिमा थी।
- बसंत (पू.) – पतझड़ गई तो बसंत आया ।
- बहार (स्त्री.) – चारों ओर वर्षा की बहार छाई थी।
- ब्रह्मपुत्र (स्त्री.) – मीलों में फैली ब्रह्मपुत्र तेज गति से बह रही थी।
- प्याज (पुं.) – उन दिनों प्याज महँगा होता जा रहा था ।
- प्यास (स्त्री.) – मुझे जोरों की प्यास लगी थी।
- फसल (स्त्री.) – खेतों में फसल लहलहा उठी।
- फागुन (पुं.) – फागुन आया और फाग के गीत गूंज उठे ।
- नींव (स्त्री.) – मकान की नींव ही कमजोर थी।
2. कर्मकारक : कर्ता द्वारा संपादित क्रिया का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़े, उसे कर्मकारक कहते हैं । इसका चिह्न ‘को’ है।
- सोहन आम खाता है। . (0-विभक्ति)
- सोहन मोहन को पीटता है । (को-विभक्ति)
यहाँ खाना (क्रिया) का फल आम पर और पीटना (क्रिया) का फल मोहन पर पड़ता है, अत: ‘आम’ और ‘मोहन’ कर्मकारक हैं।
‘आम’ के साथ ‘को’ चिह्न छिपा है और मोहन के साथ ‘को’ चिह्न स्पष्ट है। इस चिह्न का प्रयोग द्विकर्मक क्रिया रहने पर भी होता है;
- जैसेमोहन सोहन को हिन्दी पढ़ाता है । (सोहन, हिन्दी-दो कर्म)
- वह सुरेश को तबला सिखाता है । (सुरेश, तबला-दो कर्म)
3. करणकारक-जो वस्तु क्रिया के संपादन में साधन का काम करे, उसे करणकारक कहते हैं। इसका चिह्न ‘से’ है; जैसे
- मैं कलम से लिखता हूँ। (लिखने का साधन)
- वह चाकू से काटता है। (काटने का साधन)
यहाँ, ‘कलम से’, ‘चाकू से’-करणकारक हैं, क्योंकि ये वस्तुएँ क्रिया संपादन में साधन के रूप में प्रयुक्त हैं।
4. संप्रदानकारक : जिसके लिए कोई क्रिया (काम) की जाए, उसे संप्रदान कारक कहते हैं । इसका चिह्न ‘को’ और ‘के लिए’ है; जैसे
- मोहन ने सोहन को पुस्तक दी।
- मोहन ने सोहन के लिए पुस्तक खरीदी।
यहाँ पर देने और खरीदने की क्रिया सोहन के लिए है । अतः ‘सोहन को’ एवं ‘सोहन के लिए’ संप्रदानकारक हैं।
5. अपादानकारक : अगर क्रिया के संपादन में कोई वस्तु अलग हो जाए, तो उसे अपादानकारक कहते हैं । इसका चिह्न ‘से’ है; जैसे
- पेड़ से पत्ते गिरते हैं । (पेड़ से अलगाव)
- छात्र कमरे से बाहर गया । (कमरे से अलगाव)
यहाँ पेड़ से’ और ‘कमरे से’ अपादानकारक हैं, क्योंकि गिरते समय पत्ते पेड़ से और जाते समय छात्र कमरे से अलग हो गये ।
6. संबंधकारक-जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी वस्तु का संबंध जान पड़े, उसे संबंधकारक कहते हैं । इसका चिह्न ‘का’, ‘के’, ‘की’ है; जैसे
- मोहन का घोड़ा दौड़ता है।
- मोहन के घोड़े दौड़ते हैं।
- मोहन की घोड़ी दौड़ती है।
यहाँ मोहन (का, के, की) संबंधकारक हैं, क्योंकि ‘का घोड़ा’,’के घोड़े’ ‘की घोड़ी’ का संबंध मोहन से है । इसमें क्रिया से संबंध न होकर वस्तु – या व्यक्ति से रहता है।
7. अधिकरणकारक : जिससे क्रिया के आधार का ज्ञान प्राप्त हो, उसे अधिकरणकारक कहते हैं । इसका
- चिह्न ‘में’, ‘पर’ है; जैसे
- शिक्षक वर्ग में पढ़ा रहे हैं।
- महेश छत पर बैठा है।
यहाँ ‘वर्ग में’ और ‘छत पर’ अधिकरणकारक हैं, क्योंकि इनसे पढ़ाने – और बैठने की क्रिया के आधार का ज्ञान होता है।
8. संबोधनकारक : जिस शब्द से किसी के पुकारने या संबोधन का बोध हो, उसे संबोधनकारक कहते हैं । इसका चिह्न है-हे, अरे, ए आदि;. ‘जैसे
हे ईश्वर, मेरी सहायता करो। अरे दोस्त, जरा इधर आओ।
यहाँ ‘हे ईश्वर’ और ‘अरे दोस्त’ संबोधनकारक हैं । कभी-कभी संबोध नकारक नहीं भी होता है, फिर भी उससे संबोधन व्यक्त होता हैं; जैसे_ मोहन, जरा इधर आओ। भगवम्, मुझे बचाओ।
काल
काल-क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो, उसे काल कहते हैं;
जैसे
- मैंने खाया था । – (खाया था-भूत समय)
- मैं खा रहा हूँ। । – (खा रहा हूँ-वर्तमान समय)
- मैं कल खाऊँगा । – (खाऊँगा-भविष्यत् समय)
यहाँ पर क्रिया के इन रूपों-खाया था, खा रहा हूँ और खाऊँगा से भूत, वर्तमान और भविष्यत् समय (काल) का बोध होता है।
अत: काल के तीन भेद हैं-
- वर्तमामकाल (Present Tense),
- भूतकाल (Past Tense)
- भविष्यत्काल (Future Tense)
वर्तमानकाल
वर्तमानकाल : वर्तमान समय में होनेवाली क्रिया से वर्तमानकाल का बोध होता है। जैसे
- मैं खाता हूँ। – सूरज पूरब में उगता है।
- वह पढ़ रहा है। – गीता खेल रही होगी ।
वर्तमानकाल के मुख्यत: तीन भेद हैं-
- सामान्य वर्तमान
- तात्कालिक वर्तमान और
- संदिग्ध वर्तमान ।
सामान्य वर्तमान : इससे वर्तमान समय में किसी काम के करने की सामान्य आदत, स्वभाव या प्रकृति, अवस्था आदि का बोध होता है; जैसे
- कुत्ता मांस खाता है। – (प्रकृति)
- मैं रात में रोटी खाता हूँ। – (आदत)
- पिताजी हमेशा डाँटते हैं। (स्वभाव)
- वह,बहुत दुबला है। – (अवस्था)
तात्कालिक वर्तमान : इससे वर्तमान में किसी कार्य के लगातार जारी रहने का बोध होता है; जैसे
- कुत्ता मांस खा रहा है। – (खाने की क्रिया जारी है ।)
- पिताजी डाँट रहे हैं। – (इसी क्षण, कहने के समय)
संदिग्ध वर्तमान : इससे वर्तमान समय में होनेवाली क्रिया में संदेह या
अनुमान का बोध होता है; जैसे
- अमिता पढ़ रही होगी । (अनुमान)
- माली फूल तोड़ता होगा । (संदेह या अनुमान)
भूतकालं
भूतकाल : बीते समय में घटित क्रिया से भूतकाल का बोध होता है;
- जैसे
- मैंने देखा ।
- वह लिखता था ।
- राम ने पढ़ा होगः ।
- मैंने देखा है।
- वह लिख रहा था ।
- वह आता, तो मैं जाता।’
- मैं देख चुका हूँ वह लिख चुका था।
भूतकाल के छह भेद हैं
- सामान्य भूत
- आसन्न भूत
- पूर्ण भूत
- अपूर्ण भूत
- संदिग्ध भूत और
- हेतुहेतुमद् भूत ।
सामान्य भूत : इससे मात्र इस बात का बोध होता है कि बीते समय में कोई काम सामान्यतः समाप्त हुआ; जैसे
- मैंने पत्र लिखा । – (बीते समय में)
- वे पटना गये। – (बीते समय में, कब गये पता नहीं)
आसन्न भूत : इससे बीते समय में क्रिया के तुरंत या कुछ देर पहले समाप्त होने का बोध होता है, जैसे-.”
मैं खा चुका हूँ। – (कुछ देर पहले, पेट भरा हुआ है )
बैठना, जाना, बैठ जाना, हँसना, देना, हँस देना, जगना, जगाना, जगवाना आदि । … यौगिक धातु तीन प्रकार से बनता है
1. मूल धातु एवं मूल धातु के संयोग से जो यौगिक धातु बनता है, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं । जैसेमूल धातु + मूल धातु – यौगिक धातु
- हँस + दे = हँस देना
- खा + जा = खा जाना संयुक्त क्रिया
- चल + पड़ = चल पडना ।
2. मूल धातु में प्रत्यय लगने से जो यौगिक धातु बनता है, वह अकर्मक या सकर्मक या प्रेरणार्थक क्रिया होती हैं । जैसे
- मूल धातु + प्रत्यय = यौगिक धातु
- जग + ना = जगना (अकर्मक क्रिया)
- जग + आना = जगाना (सकर्मक क्रिया)
- जग + वाना = जगवाना (प्रेरणार्थक क्रिया)
3. संज्ञा, विशेषण आदि शब्दों में प्रत्यय लगने से जो यौगिक धातु बनता . है, उसे नाम-धातु कहते हैं । जैसे
- संज्ञा । विशेषण + प्रत्यय = यौगिक धातु
- हाथ (संज्ञा) + इयाना = हथियाना नाम-धातु
- गरम (विशेषण + आना = गरमाना
क्रिया के भेद
क्रिया के मुख्यतः दो भेद हैं-
(1) सकर्मक क्रिया (Transitive Verb) और (2) अकर्मक क्रिया (Intransitive Verb)।
सकर्मक क्रिया – जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म के रहने की संभावना हो, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे
खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, गाना, बजाना, मारना, पीटना आदि ।
उदाहरण:
- वह आम खाता है।
- प्रश्न : वह क्या खाता है ?
- उत्तर : वह आम खाता है।
- यहाँ कर्म (आम) है, या किसी-न – किसी कर्म के रहने की संभावना है, अतः ‘खाना’ सकर्मक क्रिया है।
अकर्मक क्रिया – जिस क्रिया के साथ कर्म न हो या कर्म के रहने की संभावना न हो, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं: जैसे
आना, जाना, हँसना, रोना, सोना, जगना, चलना, टहलना आदि।
उदाहरण :
- वह रोता है।
- प्रश्न : वह क्या रोता है?
- ऐसा न तो प्रश्न होगा और न इसका कुछ उत्तर ।
- यहाँ कर्म कुछ नहीं है और न किसी कर्म के रहने की संभावना है, अत: ‘रोना’ अकर्मक क्रिया है। .
अपवाद लेकिन कुछ अकर्मक क्रियाओं-रोना, हँसना, जगना, सोना, टहलना आदि में प्रत्यय जोड़कर सकर्मक बनाया जाता है। जैसे रुलाना, हँसाना, जगाना, सुलाना, टहलाना आदि ।
अकर्मक क्रिया + प्रत्यय – सकर्मक क्रिया
रो (ना) + लाना = रुलाना (वह बच्चे को रुलाता है ।)
जग (ना) + आना = जगाना (वह बच्चे को जगाता है।
प्रश्न : वह किसे रुलाता / जगाता है?
उत्तर : वह बच्चे को रुलाता / जगाता है।
स्पष्ट है कि रुलाना, जगाना सकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसके साथ कर्म (बच्चा है या किसी-न-किसी कर्म के रहने की संभावना है।
क्रिया के अन्य भेद
सहायक क्रिया-मुख्य क्रिया की सहायता करनेवाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं; जैसे-हूँ, है, हैं, रहा, रही, रहे, था, थे, थी, थीं आदि ।
उदाहरण:
- मैं खा रहा हूँ। – (रहा हूँ-सहायक क्रिया)
- वह पढता है। – (है-सहायक क्रिया)
यहाँ मुख्य क्रिया ‘खाना’ और ‘पढ़ना’ है जिसकी सहायता सहायक क्रिया कर रही है। –
मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के संबंध में कुछ और बाते हैं जिन्हें समझना आवश्यक है
1. किसी वाक्य में सहायक क्रिया हो या न हो, एक मुख्य क्रिया अवश्य होती है; जैसे
- वह पटना गया । (गया-मुख्य क्रिया)
- उसने शुभम् से कहा । (कहा-मुख्य क्रिया) .
2. हूँ, है, हैं, था, थे, थी, थीं, आदि सहायक क्रियाएँ हैं, लेकिन किसी वाक्य में कोई दूसरी क्रिया न हो, तो ये मुख्य क्रिया बन जाती हैं।
जैसे-
- मैं खाता हूँ। (हूँ-सहायक क्रिया)
- मैं अच्छा हूँ। (हूँ-मुख्य क्रिया)
- उसने खाया है। (है-सहायक क्रिया)
- उसे एक कलम है। (है-मुख्य क्रिया)
3. संयुक्त क्रिया में प्रथम क्रिया मुख्य क्रिया होती है और बाकी सहायता करनेवाली क्रिया सहायक क्रिया; जैसे
- वह बैठ गया था । (बैठ गया-संयुक्त क्रिया)
- यहाँ ‘बैठ’ (बैठना) मुख्य क्रिया है । ‘गया’ (जाना) और ‘था’ सहायक क्रियाएँ हैं।
नोट-गा, गे, गी को कुछ लोग भ्रमवश सहायक क्रिया समझते हैं, लेकिन ये सहायक क्रियाएँ नहीं हैं । ये प्रत्यय हैं । जैसे
मैं खाऊँगा । (मुख्य क्रिया-खाना) (सहायक क्रिया-0)
ऊपर प्रयुक्त ‘खाऊँगा” क्रिया में मूल धातु ‘खा’ है और इसमें दो प्रत्यय जुड़े हुए हैं-‘ऊँ’ एवं ‘गा’।
अर्थात्-खा (मूल धातु) + ऊँ (प्रत्यय) + गा (प्रत्यय) – खाऊँगा
पूर्वकालिक क्रिया-जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर उसी क्षण कोई दूसरी क्रिया आरंभ करता है, तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है; जैसे
खाकर, पढ़कर, लिखकर, सोकर, जगकर, आकर, जाकर आदि ।
उदाहरण:
- खाकर वह सोने गया । – (खांकर-पूर्वकालिक क्रिया)
- भाषण देकर वह बैठ गया । – (देकर-पूर्वकालिक क्रिया) .
वाच्य
वाच्य : कर्ता, कर्म या भाव (क्रिया) के अनुसार क्रिया के रूप परिवर्तन को वाच्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में, वाक्य में किसकी प्रधानता है, अर्थात्-क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष; कर्ता के अनुसार होगा, या कर्म के अनुसार होगा, या स्वयं भाव के अनुसार; इसका बोध वाच्य है;
जैसे- राम रोटी खाता है । (कर्ता के अनुसार क्रिया)-कर्ता की प्रधानता । यहाँ कर्ता के अनुसार क्रिया का अर्थ है-राम (कर्ता) – खाता है (क्रिया)
- राम – पुलिंग, एकवचन, अन्यपुरुष
- खाता है – पुलिंग, एकवचन, अन्यपुरुष
- राम ने रोटी खायी । (कर्म के अनुसार क्रिया)-कर्म की प्रधानता
- यहाँ कर्म के अनुसार क्रिया का अर्थ है – रोट (कर्म) = खायी (क्रिया)
- रोटी-स्त्रीलिंग, एकवचन, अन्यपुरुष
- खायी-स्त्रीलिंग, एकवचन, अन्यपुरुष
सीता से चला नहीं जाता । (भाव के अनुसार क्रिया)-भाव की प्रधानता।
यहाँ भाव (क्रिया) के अनुसार क्रिया का अर्थ है- चला (भाव या क्रिया) जात-(क्रिया)
- चला-पुलिंग, एकवचन, अन्यपुरुष
- जाता-पुलिंग, एकवचन, अन्यपुरुष ।
वाच्य के भेद-वाच्य के तीन भेद हैं-1. कर्तृवाच्य (Active Voice)
2. कर्मवाच्य (Passive Voice) और 3. भाववाच्य (Impersonal Voice)।
कर्तृवाच्य – कर्ता के अनुसार यदि क्रिया में परिवर्तन हो, तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं । जैसे
कर्ता – कर्म – क्रिया
- राम – (रोटी) – खाता है।
- सीता – (भात) – खाती है। कर्ता के अनुसार क्रिया-कर्तृवाच्य
- लड़के – (संतरा) – खाते हैं।
हाँ क्रियाएँ – खाता है, खाती है, खाते हैं; कर्ता के अनुसार आयीं हैं, क्योंकि यहाँ कर्ता की प्रधानता है, अत: यह कर्तृवाच्य हुआ ।
कर्मवाच्य : कर्म के अनुसार यदि क्रिया में परिवर्तन हो, तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे
कर्ता – कर्म – क्रिया
- (राम ने) – रोटी – खायी।
- (सीता ने) – भात – खाया। कर्म के अनुसार क्रिया-कर्मवाच्य
- (गीता ने) – संतरे – खाये ।
यहाँ क्रियाएँ-खायी, खाया, खाये; कर्म के अनुसार आयीं हैं. क्योंकि यहाँ कर्म की प्रधानता है, अत: यह कर्मवाच्य हुआ।
भाववाच्य : भाव (क्रिया) के अनुसार यदि क्रिया आए, तो उसे भाववाच्य कहते हैं ।
जैसे-
कर्ता भाव – (क्रिया) – क्रिया
राम से – चला नहीं – जाता।
सीता से – चला नहीं – जाता।
लड़कों से – चला नहीं – जाता।
यहाँ क्रियाएँ-जाता, जाता, जाता; भाव (क्रिया) के अनुसार आयीं हैं, क्योंकि यहाँ भाव (क्रिया) की प्रधानता है, अतः यह भाववाच्य हुआ।
उपसर्ग
प्रश्न 1.
उपसर्ग किसे कहते हैं ?
उत्तर:
उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी ‘शब्द’ के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देता है।
उपसर्ग और उनसे बने शब्द
संस्कृत के उपसर्ग

हिन्दी के उपसर्ग

उर्दू के उपसर्ग

उपसर्ग की तरह प्रयुक्त संस्कृत अव्यय

प्रत्यय
प्रश्न 1. प्रत्यय किसे कहते हैं ?
उत्तर:
ऐसे शब्दांशों को जो किसी शब्द के अन्त में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहा जाता है।
प्रश्न 2.
प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं ?
उत्तर:
प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं।
1. कृत् प्रत्यय-जो ‘प्रत्यय’ क्रिया के मूलधातु में लगते हैं, उन्हें कृत् प्रत्यय कहा जाता है । कृत् प्रत्यय से बने शब्द को ‘कृदन्त’ कहा जाता है। जैसे- पढ़नेवाला, बढ़िया, घटिया, पका हुआ, सोया हुआ, चलनी, करनी, धौकनी, मारनहारा, गानेवाला इत्यादि ।
2. तद्धित प्रत्यय-जो प्रत्यय संज्ञा और विशेषण के अन्त में लगकर उनके अर्थ में ‘परिवर्तन’ ला देते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। जैसे-सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, लकड़हारा, मनिहारा, पनिहारा, वैज्ञानिक, राजनैतिक आदि ।
विशेषण में तद्रित प्रत्यय
विशेषण में तद्धित प्रत्यय जोड़ने से भाववाचक संज्ञा बनती है । जैसे
- बुद्धिमत् + ता = बुद्धिमत्ता.
- गुरु + अ = गौरव
- लघु + त्व = लघुत्व
- लघु + अ = लाघव आदि ।
संज्ञा में तद्रित प्रत्यय
संज्ञाओं के अन्त में तद्धित प्रत्यय जोड़ने से विशेषण बनते हैं ।

समास
प्रश्न 1.
समास किसे कहते हैं ?
उत्तर:
दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं, उसे समास कहते हैं । जैसे-राजा का मंत्री = राजमंत्री। राज का पुत्र = राजपुत्र ।
प्रश्न 2.
समास के कितने भेद हैं ? सोदाहरण वर्णन करें।
उत्तर:
समास के छः भेद हैं।
1. तत्पुरुष समास-जिस सामासिक शब्द का अन्तिम खंड प्रधान हो, उस तत्पुरुष समास कहते हैं । जैसे-राजमंत्री, राजकुमार, राजमिस्त्री, राजरानी, ” देशनिकाला, जन्मान्ध, तुलसीकृत इत्यादि।
2. कर्मधारय समास-जिस सामासिक शब्द में विशेष्य-विशेषण और उपमान-उपमेय का मेल हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं । जैसे-चन्द्र के समान मुख = चन्द्रमुख, पीत है जो अम्बर = पीताम्बर आदि ।
3. द्विगु समास-जिस सामासिक शब्द का प्रथम खंड संख्याबोधक हो. उसे द्विगु समास कहते हैं । जैसे-दूसरा पहर = दोपहर, पाँच वटों का समाहार = पंचवटी, तीन लोकों का समूह = त्रिलोक, तीन कालों का समूह = त्रिकाल .. आदि ।
4. द्वन्द्व समास-जिस सामाजिक शब्द के सभी खंड प्रधान हों, उसे द्वन्द्व समास कहा जाता है । ‘द्वन्द्व’ सामासिक शब्द = गौरी-शंकर । भात और दाल = भात-दाल । सीता और राम = सीता-राम । माता और पिता = माता-पिता इत्यादि ।
5. बहुव्रीहि समास-जो समस्त पद अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बतलावे, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं । जैसे-जिनके सिर पर चन्द्रमा हो – चन्द्रशेखर । लम्बा है उदर जिनका = लम्बोदर (गणेशजी), त्रिशूल है जिनके पाणि में = त्रिशूलपाणि (शंकर) आदि ।
6. अव्ययीभाव समास-जिस सामासिक शब्द का रूप कभी नहीं बदलता हो, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं । जैसे-दिन-दिन = प्रतिदिन । शक्ति भर = यथाशक्ति । हर पल = प्रतिपल, जन्म भर = आजन्म । बिना अर्थ का = व्यर्थ आदि ।
स्मरणीय
नीचे दिए गए समस्त पदों का विग्रह करके समास बताइए ।
समस्त पद – विग्रह – समास

वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ और उनके शुद्ध रूप

विपरीतार्थक शब्द

पर्यायवाची शब्द

अनेकार्थवाची शब्द
- पत्र – पत्रा, चिट्ठी, पंख।
- तारा – नक्षत्र, आँख की पुतली, बाली की स्त्री, बृहस्पति की स्त्री ।
- कुल’ – समुदाय, वंश, वर्ग, योग ।
- सोना – नींद में सोना, एक मूल्यवान धातु ।।
- विधि – कानून, तरीका, ब्रह्मा, भाग्य, ईश्वर ।
- पक्ष – तरफ, पंख, पखवारा ।
- अग्र – आगे, पहले, पखवारा ।
- वर्ण – अक्षर, जाति, रंग ।
- मान – सम्मान, नाप, तौल, रूठना, घमंड ।
- पयोधर – बादल, स्तन, गन्ना, पर्वत ।
- नाक – नासिका, प्रतिष्ठा, स्वर्ग |
- दल – पत्ता, समूह ।
- जेष्ठ – बड़ा, श्रेष्ठ, जेठ का महीना, पति का बड़ा भाई ।
- चक्र – पहिया, चाक, चकवा ।
- चपला – बिजली, लक्ष्मी।
- घन – बादल, हथौड़ा, गहरा ।
- गुरु – कला, शिक्षक, भारी, बड़ा ।
- खग – पक्षी, तीर, हवा, ग्रह ।
- काल – मृत्यु, समय, यमराज, अकाल ।
- अलि – भौंरा, बिच्छू ।
श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द
- अलि – भौंरा
- आवास – रहने का स्थान
- आली – सखी
- आभास – झलक, संकेत
- क्षत्र – प्रभुत्व
- ‘छत्र – छाता
- आँगना – घर का
- आँगन अंगना – स्त्री
- अन्न – अनाज
- अन्य – दूसरा
- अम्बु – जल
- अम्ब – आम,
- माता अथक – बिना
- थके हुए पत्र – योग्य बर्तन पथ
- पौत्र – पोता
- पोत –’जहाज
- प्रण – जान, जीवन
- बली – वीर, राजा बलि
- बहन – बहिन
- भवन – महल, घर
- भुवन – संसार
- भारतीय – भारत
- का भारती – सरस्वती
- पवन – हवा
अनेक शब्दों के लिए एक शब्द
- जो मापा न जा सके – अपरिमित
- जो पहले कभी नहीं देखा गया – अदृष्टपूर्व
- जो बहुत बोलता है – वाचाल
- जो कहा गया हो – कथित
- जिसका तेज नष्ट हो गया हो – निस्तेज
- पीने योग्य – पेय
- कम बोलनेवाला – मितभाषी
- दुःख देनेवाला – दु:खद
- खाली करनेवाला – रिक्तक
- जिसके हाथ में वीणा हो – वीणापाणि
- जिसके सिर पर चन्द्रमा हो चन्द्रशेखर, – चन्द्रमौलि
- जानने की इच्छा – जिज्ञासा
- जीतने की इच्छा – जिगीषा
- जीने की इच्छा – जिजीविषा
- खाने की इच्छा – बुभुक्षा
- युद्ध करने की इच्छा – युयुत्सा
- जिसको कभी भेदा न जा सके। – अभेद्य
- जिसके आने की तिथि मालूम न हो – अतिथि
- जिसका कोई न हो – अनाथ
- मेघ की तरह नाद करनेवाला – मेघनाद
- जो दूसरो के अधीन हो – पराधीन
- जो जन्म से अन्धा हो – जन्मान्ध
- शिव का भक्त – शैव
- विष्णु का उपासक – वैष्णव
- इस लोक की बात – लौकिक
- रात में घूमनेवाला – निशाचर
- वर्ष में एक बार होनेवाला – वार्षिक
मुहावरे
जी सन्न होना (अचानक घबरा जाना)-इस बात को सुनते ही मेरा जी सन्न हो गया।
आकाश-पाताल एक करना (बहुत प्रयत्न करना) – अपने खोये हुए .. लड़के की खोज में उसने आकाश-पाताल एक कर दिया । ।
उलटे छरे से मुड़ना (बेवकूफ बनाकर लटना) – एक का तीन लेकर आज उसने उल्टे छुरे से मूड़ लिया ।
दाँत खट्टा करना (परास्त करना) – शिवाजी ने मुगलों के दाँत खट्टे कर दिये।
नाक काटना (इज्जत लेना)-भरी सभा में उसने मेरी नाक काट ली।
नाकों चने चबाना (खूब तंग करना)-आज की बहस में आपने तो मुझे – नाकों चने चबवा दिये।
अपने पाँव आप कुल्हाड़ी मारना (अपना नुकसान आप करना)-क्यों – पढ़ाई करके अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार रहे हो ?
आस्तीन में साँप पालना (दुश्मन को पालना)-मुझे क्या मालूम था कि – मैं आस्तीन में साँप पाल रहा हूँ।
आपे (पायजामा) से बाहर होना (होश खोना, घमंड करना)-क्यों – इतना आपे से बाहर हो रहे हैं, चुप रहिए
इधर की दुनिया उधर हो जाना (अनहोनी बात होना) – इधर की दुनिया – उधर भले ही जाए, पर वह पथ से विपथ नहीं होगा।
उठ जाना (खत्म होना, मर जाना, हट जाना) – आज वह संसार से उठ । गया।
ओस का मोती (क्षण भंगुर) – शरीर तो ओस का मोती है।
कलेजा मुँह को आना (दुःख से व्याकुल होना)-दुःख की खबर सुनकर उसका कलेजा मुँह को आ गया ।
काठ मार जाना (लज्जित होना) – भेद खुलते ही उसको काठ मार गया।
छाती पत्थर की करना (जी कड़ी करना) – अब मैंने उसके लिए अपनी छाती पत्थर की कर ली है।
छठी का दूध याद आना (घोर कठिनाई में पड़ना) – इस बार तो उसे छठी का दूध याद आ जाएगा । – आटे के साथ घुन पीसना (बड़े के साथ छोटे को हानि उठाना)-मैं इस मुकदमे में आटे के साथ घुन की तरह पिस रहा हूँ।
आँखें चार होना (देखा-देखी होना, प्यार होना) – सर्वप्रथम पुष्पवाटिका में राम-सीता की आँखें चार हुई थीं।
आँखें भर आना (आँसू आना) – इंदिराजी की मृत्यु की खबर सुनते ही लोगों की आँखें भर आयीं।
आँखें चुराना (सामने न आना) – परीक्षा में असफल होने पर राम पिता से आँखें चुराता रहा।
अंक भर लेना (लिपटा लेना) – माँ ने बेटी को देखते ही अंक भर लिया अंगूठा चूमना (खुशामद करना)-जब तक उसका अंगूठा नहीं चूमोगे, नौकरी नहीं मिलेगी।
अंकुश देना (दबाव डालना)-वह हर काम अंकुश देकर करवाता है। – आड़े हाथों लेना (भला-बुरा कहना)-आज भरी सभा में उसने मुझे आड़े हाथों लिया।
आकाश चूमना (बहुत ऊँचा होना) – कोलकाता के प्रायः सभी सरकारी भवन आकाश को चूमते नजर आते हैं ।
अंधेरा छाना (कोई उपाय न सूझना) – इकलौते पुत्र की अकाल मृत्यु का समाचार पाते ही उसके सामने अंधेरा छा गया ।
अपनी खिचड़ी अलग पकाना (सबसे परे रहना)-अरे मिलजुल कर रहो । अपनी खिचड़ी अलग पकाने से कोई फायदा नहीं है।
अब-तब करना (मरणासन्न होना, आना-कानी करना) – मोहन के पिता बस अब-तब कर रहे हैं । कर्ज देना. ही होगा, अब-तब करने से काम न चलेगा। ………. अक्ल का दुश्मन (मूर्ख)-यह लड़का निश्चय ही अक्ल का दुश्मन है। अक्ल के घोड़े दौड़ाना (कल्पना करना)-लाख अक्ल के घोड़े दौड़ाओ, पर यह समस्या सुलझेगी नहीं।
औचट में पड़ना (व्यर्थ में तंग होना) – बेचारा औचट में पड़ गया, उसका कोई दोष नहीं था।
आग उगलना (अतिशय क्रोध करना) – बच्चों की गलती पर भी आग उगल रहे हो।
आग में कूद पड़ना (जोखिम उठाना) – साहसी व्यक्ति हँसते-हँसते आग में भी कूद पड़ते हैं।
आँसू पीकर रह जाना (भीतर ही भीतर रोकर रह जाना)-पति के मर जाने पर चोर की स्त्री आँसू पीकर रह गयो ।
आँसू पीकर रह जाना (भीतर ही भीतर रोकर रह जाना)-पति के मर जाने पर चोर की स्त्री आँसू पीकर रह गयी ।
आसमान से बातें करना (अत्यंत ऊँचा होना)-मैनेजर बनने के बाद वह आसमान से बातें करने लगा है। आसमान के तारे तोड़ना (असंभव को संभव कर दिखाना)-गुरु के आदेश पर मैं आसमान के तारे भी तोड़ कर ला सकता हूँ।
आँचल पसारना (याचना करना)-माया ने अपने पति की रक्षा के लिए भगवान के सामने आँचल पसार दिया ।
श्रीगणेश करना (आरंभ करना)-काम का श्रीगणेश कब होगा ?
अंधा बनाना (मूर्ख बनाना)- लोगों को अंधा बनाना ही आजकल चालाकी का पर्याय बन गया है। – अपने पाँव पर खड़ा होना (आत्म-निर्भर होना)-जो व्यक्ति बीस वर्ष
की अवधि में अपने पाँव पर खड़ा होने लायक नहीं हुआ, उससे बहुत आशा नहीं करनी चाहिए।
अंगार बनना (क्रोध में आना)-नौकर के हाथ से प्याला गिरा और . मालकिन अंगार हो गयी। अंधे की लाठी (एक मात्र सहारा)-मेरा पुत्र ही मेरे लिए अंधे की लाठी ………. आँख की किरकिरी (खटकने वाला)-राम मेरी आँखों की किरकिरी है, मैं उसे निकाल कर ही दम लूँगा।
आँख की पुतली (अत्यंत प्यारी)-मैं अपनी माँ की आँखों की पुतली
ईट-से-ईंट बजाना (ध्वंस करना)-बड़े से लडोगे तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर वह तुम्हारी ईंट-से-ईंट बजा देगा।
उठा न रखना (कसर न छोड़ना)- मैं तुम्हारी भलाई के लिए कुछ न उठा रखूगा।
खेत आना (वीरगति प्राप्त होना)–पाकिस्तान के युद्ध में अनेक सैनिक खेत आये। – उल्टी गंगा बहाना (प्रतिकूल कार्य करना)-उसने इस अनुसंधान से । उल्टी गंगा बहा दी । दुष्टों को सच्चरित्र बनाना उल्टी गंगा बहाना है । . उल्लू सीधा करना (काम बना लेना)-उसने रुपये के बल पर अपना
उल्लू सीधा कर लिया। मतलबी लोग हमेशा अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं।
कागज काला करना (बेमतलब लिखे जाना)-आजकल कामज काला करने वाले ही अधिक हैं, मौलिक लेखक बहुत कम । – आटे-दाल का भाव मालूम होना (सांसारिक कठिनाइयों का ज्ञान होना)- अभी मौज कर लो, जब परिवार का बोझ सिर पर पड़ेगा तब
आटे-दाल का भाव मालूम होगा। आठ-आठ आँसू रोना (विलाप करना)-अभिमन्यु की मृत्यु पर सभी
पांडव आठ-आठ आँसू रोये । आँखें लड़ाना (नेह जोड़ना)-हर किसी से आँखें लड़ाना ठीक नहीं । – अक्ल पर पत्थर पड़ना (समय पर अक्ल चकराना)-मेरी अक्ल पर ।
पत्थर पड़ गया था कि घर में बंदूक रहते भी उसका प्रयोग न कर सका। – अंगारों पर पैर रखना (जान-बूझकर खतरा मोल लेना)-पाकिस्तान . भारत से दुश्मनी मोल लेकर अंगारों पर पैर रख रहा है ।
कागजी घोड़ा दौड़ाना (कार्यालयों की बेमतलब की लिखा-पढ़ी)-कागजी घोड़ा अधिक दौड़ाओ, काम करो, यही जमाना आ गया है।
कीचड़ उछालना (किसी की प्रतिष्ठा पर आघात करना)-बिना सोचे
अंगारों पर पैर रखना (जान-बूझकर खतरा मोल लेना)-पाकिस्तान
भारत से दुश्मनी मोल लेकर अंगारों पर पैर रख रहा है। का कागजी घोड़ा दौड़ाना (कार्यालयों की बेमतलब की लिखा-पढ़ी)-कागजी घोड़ा अधिक दौड़ाओ, काम करो, यही जमाना आ गया है ।
कीचड़ उछालना (किसी की प्रतिष्ठा पर आघात करना)-बिना सोचे -किसी पर कीचड़ उछालना अच्छा नहीं है।
कुआँ खोदना (किसी की बुराई करने का उपाय करना)-जो दूसरों के ‘लिए कुआँ खोदता है, वह स्वयं गड्ढे में गिरता है।
आँखों से पानी गिर जाना (निर्लज्ज हो जाना)-तुम अपने बड़े भाई से सवाल-जवाब करते हो, क्या तुम्हारी आँखों से पानी गिर गया है ? ..
जबान हिलाना (बोलना)-और अधिक जबान हिली तो ठीक न होगा। ठोकर खाना (हानि होना)-ठोकर खाकर ही कोई सीखता है। दंग रह जाना (चकित होना)-मैं तो उसका खेल देखकर दंग रह गया। धौंस में आना (प्रभाव में आना)-तुम्हारी धौंस में हम आने वाले नहीं
धज्जियाँ उड़ाना (टुकड़े-टुकड़े कर डालना, खूब मरम्मत करना, किसी का भेद खोलना)-भरी सभा में उसकी धज्जियाँ उड़ गयीं। – पत्थर की लकीर (अमिट)-मेरी बात पत्थर की लकीर समझो।
पानी फेरना (नष्ट करना)-उसने सब किये-धरे पर पानी फेर दिया । पीछे पड़ना (लगातार तंग करना)-क्यों मेरे पीछे पड़े हो भाई । गम खाना (दबाना)-बेचारा डर के मारे गम खाकर रहता है । खाक छानना (भटकना)-वह नौकरी की खोज में खाक छानता रहा । रंग जमाना (धाक जमाना)-आपने अपना रंग जमा लिया । करवट बदलना (बेचैन रहना)-मैं सारी रात करवटें बदलता रहा ।
काम तमाम करना (खत्म करना)-मैंने आज अपने दुश्मन का काम तमाम कर दिया। कचूमर निकालना (खूब पीटना)-पुलिस वालों ने चोरों को मारते-मारते उनके कचूमर निकाल दिये। .न घर का न घाट का (किसी लायक नहीं)-नौकरी छूटने के बाद वह न घर का रहा न घाट का ।
खार खाना (डाह करना)-न मालूम वे मुझसे क्यों खार खाये बैठे हैं ? – गोटी लाल होना (लाभ होना)-अब क्या है, तुम्हारी गोटी लाल है।
गड़े मुर्दे उखाड़ना (दबी बात को फिर से उभारना)-समझौता-वार्ता में गड़े मुर्दे मत उखाड़िए।
गुड़ गोबर करना (बना-बनाया काम बिगाड़ना)-आज आपने सब गुड़ गोबर कर दिया।
घी के दिये जलाना (अति प्रसन्नता प्रकट करना)-तुम इस परीक्षा में सफल हो जाओ तो मैं घी के दिये जलाऊँ ।
चाँद पर थूकना (बड़े आदमी पर कलंक लगाना)-गाँधीजी को गलत कहना चाँद पर थूकना है।
चम्पत होना (भाग जाना)-घर में जो कुछ मिला उसे लेकर चोर चम्पत हो गया। _चाँदी काटना (सुख से जिंदगी बसर करना)-अब बुढ़ापे में वह चाँदी काट रहा है।
तेवर बदलना (क्रोध करना)-बात-बात में वह तेवर बदला करता है। ” तूती बोलना (खूब चलना)-आजकल तो सर्वत्र कांग्रेस पार्टी की तूती । बोल रही है। तीन-तेरह होना (तितर-बितर होना)-मुगलों की सारी सेना तीन-तेरह हो गयी। – दूज का चाँद होना (कम दर्शन देना)-आजकल तो आप दूज के चाँद हो गये हैं।
बाग-बाग होना (अति खुश होन्ग्र)-यह दृश्य देखते ही मैं बाग-बाग हो गया।
नौ-दो ग्यारह होना (भाग जाना)-पुलिस को देखते ही चोर नौ-दो ग्यारह हो गये। पापड़ बेलना (प्रयत्नों का निरर्थक होना)-क्या यों ही पापड़ बेलते सारी
उम्र कटेगी? – लाले पड़ना (पूर्ण अभाव होना)-इन दिनों यहाँ अन्न के लाले पड़े हैं।
हाथ के तोते उड़ना (स्तब्ध होना)-फेल होने का समाचार सुनकर उसके हाथ के तोते उड़ गये।
सब्जबाग दिखाना (बड़ी-बड़ी आशाएँ दिलाना)-उसने अपना काम निकालने के लिए जनता को सब्जबाग दिखाया। लाल-पीला होना (रंज होना)-आप व्यर्थ ही मुझ पर लाल पीले हो रहे
हैं, मेरा तो कसूर कुछ नहीं है। – पौ बारह होना (खूब लाभ होना)-इन दिनों उनके पौ बारह हैं। … – पानी-पानी
होना (अत्यंत लज्जित होना)-अपनी मूर्खता पर वह पानी-पानी
हो गया। . मुँह की खाना (बुरी तरह हारना)-अंत में उसने मुँह की खायी। – छक्के छुड़ाना (हिम्मत पस्त करना)-शिवाजी ने औरंगजेब के छक्के छुड़ा दिये।
BSEB Textbook Solutions PDF for Class 8th
- BSEB Class 8 Textbook Solutions PDF: Download Bihar Board STD 8th Book Answers
- BSEB Class 8 Hindi Textbook Solutions PDF: Download Bihar Board STD 8th Hindi Book Answers
- BSEB Class 8 Hindi Chapter 1 तू जिन्दा है तो Textbook Solutions PDF: Download Bihar Board STD 8th Hindi Chapter 1 तू जिन्दा है तो Book Answers
- BSEB Class 8 Hindi Chapter 2 ईदगाह Textbook Solutions PDF: Download Bihar Board STD 8th Hindi Chapter 2 ईदगाह Book Answers
- BSEB Class 8 Hindi Chapter 3 कर्मवीर Textbook Solutions PDF: Download Bihar Board STD 8th Hindi Chapter 3 कर्मवीर Book Answers
- BSEB Class 8 Hindi Chapter 4 बालगोबिन भगत Textbook Solutions PDF: Download Bihar Board STD 8th Hindi Chapter 4 बालगोबिन भगत Book Answers
- BSEB Class 8 Hindi Chapter 5 हुंडरू का जलप्रपात Textbook Solutions PDF: Download Bihar Board STD 8th Hindi Chapter 5 हुंडरू का जलप्रपात Book Answers
- BSEB Class 8 Hindi Chapter 6 बिहारी के दोहे Textbook Solutions PDF: Download Bihar Board STD 8th Hindi Chapter 6 बिहारी के दोहे Book Answers
- BSEB Class 8 Hindi Chapter 7 ठेस Textbook Solutions PDF: Download Bihar Board STD 8th Hindi Chapter 7 ठेस Book Answers
- BSEB Class 8 Hindi Chapter 8 बच्चे की दुआ Textbook Solutions PDF: Download Bihar Board STD 8th Hindi Chapter 8 बच्चे की दुआ Book Answers
- BSEB Class 8 Hindi Chapter 9 अशोक का शास्त्र-त्याग Textbook Solutions PDF: Download Bihar Board STD 8th Hindi Chapter 9 अशोक का शास्त्र-त्याग Book Answers
- BSEB Class 8 Hindi Chapter 10 ईर्ष्या : तू न गई मेरे मन से Textbook Solutions PDF: Download Bihar Board STD 8th Hindi Chapter 10 ईर्ष्या : तू न गई मेरे मन से Book Answers
- BSEB Class 8 Hindi Chapter 11 कबीर के पद Textbook Solutions PDF: Download Bihar Board STD 8th Hindi Chapter 11 कबीर के पद Book Answers
- BSEB Class 8 Hindi Chapter 12 विक्रमशिला Textbook Solutions PDF: Download Bihar Board STD 8th Hindi Chapter 12 विक्रमशिला Book Answers
- BSEB Class 8 Hindi Chapter 13 दीदी की डायरी Textbook Solutions PDF: Download Bihar Board STD 8th Hindi Chapter 13 दीदी की डायरी Book Answers
- BSEB Class 8 Hindi Chapter 14 पीपल Textbook Solutions PDF: Download Bihar Board STD 8th Hindi Chapter 14 पीपल Book Answers
- BSEB Class 8 Hindi Chapter 15 दीनबन्धु ‘निराला’ Textbook Solutions PDF: Download Bihar Board STD 8th Hindi Chapter 15 दीनबन्धु ‘निराला’ Book Answers
- BSEB Class 8 Hindi Chapter 16 खेमा Textbook Solutions PDF: Download Bihar Board STD 8th Hindi Chapter 16 खेमा Book Answers
- BSEB Class 8 Hindi Chapter 17 खुशबू रचते हैं हाथ Textbook Solutions PDF: Download Bihar Board STD 8th Hindi Chapter 17 खुशबू रचते हैं हाथ Book Answers
- BSEB Class 8 Hindi Chapter 18 हौसले की उड़ान Textbook Solutions PDF: Download Bihar Board STD 8th Hindi Chapter 18 हौसले की उड़ान Book Answers
- BSEB Class 8 Hindi Chapter 19 जननायक कर्पूरी ठाकुर Textbook Solutions PDF: Download Bihar Board STD 8th Hindi Chapter 19 जननायक कर्पूरी ठाकुर Book Answers
- BSEB Class 8 Hindi Chapter 20 झाँसी की रानी Textbook Solutions PDF: Download Bihar Board STD 8th Hindi Chapter 20 झाँसी की रानी Book Answers
- BSEB Class 8 Hindi Chapter 21 चिकित्सा का चक्कर Textbook Solutions PDF: Download Bihar Board STD 8th Hindi Chapter 21 चिकित्सा का चक्कर Book Answers
- BSEB Class 8 Hindi Chapter 22 सुदामा चरित Textbook Solutions PDF: Download Bihar Board STD 8th Hindi Chapter 22 सुदामा चरित Book Answers
- BSEB Class 8 Hindi Chapter 23 राह भटके हिरन के बच्चे को Textbook Solutions PDF: Download Bihar Board STD 8th Hindi Chapter 23 राह भटके हिरन के बच्चे को Book Answers
- BSEB Class 8 Hindi व्याकरण Textbook Solutions PDF: Download Bihar Board STD 8th Hindi व्याकरण Book Answers
- BSEB Class 8 Hindi निबंध लेखन Textbook Solutions PDF: Download Bihar Board STD 8th Hindi निबंध लेखन Book Answers
- BSEB Class 8 Hindi पत्र-लेखन Textbook Solutions PDF: Download Bihar Board STD 8th Hindi पत्र-लेखन Book Answers






0 Comments:
Post a Comment